
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 1
January 2026
Indexing Partners
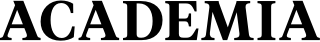




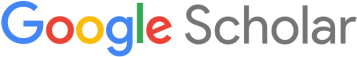








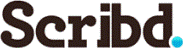




भारत में सम्राट अशोक का ऐतिहासिक योगदान: एक शोधात्मक अध्ययन
| Author(s) | Aravind |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का व्यक्तित्व एक ऐसे शासक का उदाहरण है, जिसने सत्ता के शिखर पर पहुँचने के बाद आत्मबोध और नैतिक चेतना के आधार पर न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की दिशा बदली, बल्कि शासन की परिभाषा और उद्देश्य को भी पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। मौर्य वंश के इस तीसरे शासक ने प्रारंभ में अपने पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति सैन्य विस्तार और शक्ति के माध्यम से साम्राज्य को दृढ़ किया, लेकिन कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) के बाद उनके जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वह इतिहास में अभूतपूर्व है। कलिंग युद्ध की विभीषिका, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों निर्वासित हुए, अशोक के अंतर्मन को झकझोर गई। यह युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना, जहाँ से एक हिंसक विजेता के स्थान पर एक नैतिक शासक का जन्म हुआ। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को अपनाया, बल्कि एक ऐसे 'धम्म' या नैतिक नीति को जीवन और शासन का आधार बनाया, जो धर्मनिरपेक्ष, करुणामूलक और लोकहितकारी था। अशोक का यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल प्रशासनिक दक्षता या सैन्य विजय में नहीं होता, बल्कि उसमें आत्मानुशासन, नैतिकता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश भी आवश्यक होता है। उन्होंने ‘धम्म विजय’ को ‘राजनैतिक विजय’ से अधिक महत्व दिया और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसमें शासक प्रजा का हितैषी और मार्गदर्शक होता है, न कि केवल आदेश देने वाला राजा। अशोक के समय भारत का भूगोल अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कर्नाटक तक विस्तृत था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, बौद्ध विचारधारा का वैश्विक प्रसार और प्रशासन में नैतिक मूल्यों की स्थापना थी। उनके अभिलेख और शिलालेख आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में उनके संदेश को जीवंत बनाए हुए हैं। यह शोधपत्र सम्राट अशोक के इसी बहुआयामी योगदान का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है — जहाँ एक विजेता शासक धीरे-धीरे मानवतावादी नेता में बदलता है, और अपनी आत्मशक्ति को जनता की सेवा, नैतिक मूल्यों के प्रसार और वैश्विक शांति के लिए समर्पित करता है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय प्रतीकों में आज भी अशोक की उपस्थिति, उनके ऐतिहासिक योगदान की चिरस्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। इस शोध अध्ययन के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अशोक के व्यक्तित्व और कार्यों ने न केवल उनके समकालीन समाज को दिशा दी, बल्कि आधुनिक भारत की विचारधारा और नीतियों को भी गहराई से प्रभावित किया। उनके जीवन से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य, शासन व्यवस्था, धर्मनीति और विश्व को दिए गए संदेश — सभी आज के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और नैतिक शासन के आदर्शों के निकटतम उदाहरण हैं। 2. शोध उद्देश्य (Objectives of the Study) इस शोध का मुख्य उद्देश्य सम्राट अशोक के ऐतिहासिक योगदान का गहन, समग्र और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अशोक केवल मौर्य साम्राज्य के विस्तारवादी शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने शासन की उस नैतिक दिशा को प्रस्तुत किया जो आज भी शासन-प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रेरणास्रोत मानी जाती है। निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से इस शोध में अशोक के विविध पक्षों का परीक्षण किया जाएगा: 1. सम्राट अशोक के राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना: इस उद्देश्य के अंतर्गत अशोक की साम्राज्य विस्तार नीति, उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक संरचना, अधिकारियों की नियुक्ति, 'धम्म महामात्र' जैसे विशेष पदों की भूमिका, प्रजा से संवाद के साधन तथा शासन को लोकहितकारी बनाने की उनकी नीति का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही यह देखा जाएगा कि उनके राजनीतिक निर्णय किस हद तक नैतिक मूल्यों से प्रेरित थे। 2. अशोक द्वारा अपनाई गई धर्मनीति (धम्म) के ऐतिहासिक प्रभावों का विश्लेषण करना: अशोक का ‘धम्म’ किसी संप्रदाय विशेष की संकीर्ण विचारधारा न होकर एक सार्वभौमिक नैतिकता पर आधारित जीवन दृष्टि थी। इस उद्देश्य के अंतर्गत उनके धम्म के सिद्धांत, उसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजाहित में अपनाए गए उपायों तथा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझने का प्रयास किया जाएगा। 3. अशोक के शिलालेखों और स्तंभलेखों के माध्यम से उनकी नीतियों और दर्शन को समझना: अशोक ने अपने विचारों, नीतियों और धम्म सन्देशों को शिलालेखों के माध्यम से प्रचारित किया। इस उद्देश्य के अंतर्गत इन अभिलेखों का विश्लेषण करते हुए यह जाना जाएगा कि वे उनके शासन के औचित्य, नैतिक दायित्व, प्रजाहित एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नीति का दर्पण कैसे हैं। साथ ही लिपि, भाषा और भौगोलिक वितरण का भी अध्ययन किया जाएगा। 4. भारत और एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में अशोक के योगदान का मूल्यांकन करना: अशोक ने बौद्ध धर्म के अंतरराष्ट्रीय प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में बौद्ध मिशनरियों को श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, यूनान तक भेजा गया। इस उद्देश्य के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाएगा कि अशोक के प्रभाव से बौद्ध धर्म किस प्रकार एशियाई सांस्कृतिक सेतु के रूप में विकसित हुआ। 5. अशोक की शासन शैली का आधुनिक शासन व्यवस्थाओं पर प्रभाव का आकलन करना: सम्राट अशोक की शासन नीति ने सेवा, संवाद, सहिष्णुता और नैतिकता को प्राथमिकता दी। इस उद्देश्य के अंतर्गत यह विश्लेषण किया जाएगा कि कैसे अशोक की नीतियाँ आधुनिक लोकतांत्रिक शासन, नीति निर्माण, प्रशासनिक आचरण और सार्वजनिक जीवन के मूल्यों पर प्रभाव डालती हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में अशोक स्तंभ और अशोक चक्र की उपस्थिति के माध्यम से उनके योगदान की समकालीन प्रासंगिकता को भी समझा जाएगा। इन सभी उद्देश्यों के माध्यम से यह शोध न केवल अशोक की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि क्यों उन्हें भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी शासक के रूप में स्मरण किया जाता है। 3. शोध पद्धति (Research Methodology) यह शोध कार्य मुख्यतः गुणात्मक (Qualitative) एवं ऐतिहासिक-समीक्षात्मक (Historical-Analytical) पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सम्राट अशोक के जीवन, शासन प्रणाली, धम्म दर्शन, और उनके ऐतिहासिक योगदान को साक्ष्य आधारित और वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करना है। इस पद्धति में न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, बल्कि उनके पीछे की वैचारिक प्रवृत्तियों, सामाजिक प्रभावों और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रकृति का विश्लेषण भी किया गया है। शोध में निम्नलिखित स्रोतों और तकनीकों का समावेश किया गया है: 1. प्राथमिक स्रोतों का उपयोग • शिलालेख एवं स्तंभलेख: अशोक द्वारा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में उत्कीर्ण शिलालेख (जैसे धौली, गिरनार, सारनाथ, लौरिया-नंदनगढ़ आदि) इस शोध के प्रमुख स्त्रोत हैं। इन लेखों से न केवल धम्म की अवधारणा, अपारधर्म निंदा, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व, और धार्मिक सहिष्णुता के संकेत मिलते हैं, बल्कि तत्कालीन शासन तंत्र, प्रशासनिक दृष्टिकोण और अशोक के व्यक्तिगत चिंतन का भी अनुमान लगाया जा सकता है। • ताम्रपत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्य: अशोक कालीन मुद्राएं, मूर्तिकला, स्थापत्य और पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से मौर्यकालीन संस्कृति और प्रशासन की जानकारी प्राप्त की गई है। • बौद्ध ग्रंथ: दीघ निकाय, महावंश, दीपवंश जैसे बौद्ध साहित्य से अशोक के जीवन, धम्म प्रचार और बौद्ध धर्म अंगीकरण के संदर्भ मिलते हैं। 2. द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण • इतिहासकारों के ग्रंथ: समकालीन और आधुनिक इतिहासकारों जैसे रोमिला थापर, नयनजोत लाहिरी, डी.एन. झा, ए.एल. बाशम आदि के शोध-पत्र, पुस्तकों और विश्लेषणों का उपयोग किया गया है। • शोध पत्र और समीक्षात्मक लेख: विभिन्न अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से अशोक के शासन और धम्म के आधुनिक मूल्यांकन की दृष्टि प्राप्त की गई है। • विदेशी यात्रियों की टिप्पणियाँ: यद्यपि अशोक के समकालीन विदेशी यात्रियों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु चीनी यात्री फा-ह्यान और ह्वेनसांग की टिप्पणियाँ बाद के बौद्ध प्रभाव और अशोक स्तंभों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। 3. तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया • अशोक के शासन की तुलना समकालीन और पूर्ववर्ती शासकों — जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर महान, तथा अन्य एशियाई सम्राटों की नीतियों से की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अशोक का शासन किस रूप में विशिष्ट और क्रांतिकारी था। • उनके धम्म-दर्शन की तुलना जैन और बौद्ध नैतिक मूल्यों के साथ करते हुए यह देखा गया है कि कैसे अशोक ने भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक समावेशी रूप प्रस्तुत किया। 4. मूल्यांकनात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण • इस शोध में Contextual Analysis और Textual Interpretation की विधियों का उपयोग कर शिलालेखों के पाठों की व्याख्या की गई है। • अशोक की नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव का भी ऐतिहासिक क्रम में विश्लेषण किया गया है — विशेषकर आधुनिक भारतीय प्रतीकों (अशोक स्तंभ, अशोक चक्र) में उनकी उपस्थिति के आलोक में। इस प्रकार, यह शोध इतिहास को केवल घटनाओं के संकलन के रूप में नहीं, बल्कि उसके पीछे के वैचारिक, नैतिक और सांस्कृतिक विमर्श को उजागर करने का प्रयास है। अशोक के योगदान का समग्र अध्ययन तभी संभव है जब हम साक्ष्यों, व्याख्याओं और ऐतिहासिक प्रभावों का एक साथ विश्लेषण करें, जिसे इस शोध कार्य में सुनिश्चित किया गया है। 4. अशोक का प्रारंभिक शासन और कलिंग युद्ध सम्राट अशोक का प्रारंभिक शासनकाल मौर्य वंश की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें साम्राज्य विस्तार, सैन्य शक्ति और केन्द्रीय नियंत्रण को सर्वोच्च माना जाता था। उनके पिता बिंदुसार और पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक ने युवराज बनने के बाद से ही प्रशासनिक दक्षता और सैन्य नेतृत्व का परिचय देना शुरू कर दिया था, परंतु सम्राट बनने की उनकी राह सहज नहीं थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि अशोक को सत्ता प्राप्ति के लिए अपने सौतेले भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इस सत्ता संघर्ष में उन्होंने कथित रूप से कई भाइयों को पराजित कर राजगद्दी प्राप्त की। यह घटनाक्रम न केवल मौर्य सत्ता के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि अशोक प्रारंभ में एक निर्णायक, कठोर और महत्वाकांक्षी शासक थे। शासनारूढ़ होने के कुछ वर्षों बाद अशोक ने पूर्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और कलिंग (वर्तमान उड़ीसा) पर आक्रमण किया, जो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था। 261 ई.पू. में हुआ यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। कलिंग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण था, परंतु इस युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या, उजड़े परिवार, और सामाजिक विनाश ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। उनके शिलालेखों में यह उल्लेख मिलता है कि — “कलिंग युद्ध में एक लाख से अधिक लोग मारे गए, डेढ़ लाख बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग युद्ध और उसके परिणामों से पीड़ित हुए।” इस भयानक नरसंहार और उसके बाद जनमानस में उत्पन्न पीड़ा ने अशोक को आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त किया। यही वह क्षण था जब एक विजेता सम्राट के भीतर करुणा का बीज अंकुरित हुआ, और उन्होंने अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। अशोक के लिए यह परिवर्तन केवल भावनात्मक या व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनकी पूरी शासन-नीति, विचारधारा और सार्वजनिक जीवन का आधार बन गया। यहीं से आरंभ होता है उनका ‘धम्म मार्ग’ — जो भविष्य के शासकों के लिए नैतिकता और मानवता की मिसाल बन गया। 5. धर्म-परिवर्तन और धम्म नीति कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने जिस धर्म को अपनाया, वह पारंपरिक अर्थों में केवल बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि एक समन्वित नैतिक जीवन पद्धति थी, जिसे उन्होंने 'धम्म' कहा। अशोक का धम्म किसी एक धार्मिक पंथ या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह भारतीय परंपराओं में निहित सत्य, अहिंसा, दया, संयम, और करुणा जैसे गुणों का सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में अनुसरण करने का आह्वान था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर यह स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म वही है जो आत्मानुशासन, सहिष्णुता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ावा दे। उन्होंने यह भी कहा कि “सच्ची पूजा, ब्राह्मणों और श्रमणों का सम्मान करना, माता-पिता की सेवा, प्राणियों पर दया और सत्य भाषण है।” उनकी धम्म नीति में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों को विशेष स्थान प्राप्त था: • धार्मिक सहिष्णुता: अशोक सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते थे। उन्होंने बार-बार अपने शिलालेखों में इस बात पर ज़ोर दिया कि विभिन्न मतों और विचारधाराओं का आदान-प्रदान समाज के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक है। • नैतिक जीवन मूल्यों का प्रचार: जैसे सत्य, दया, संयम, ईर्ष्या का परित्याग, गपशप से बचना, और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना। • पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों की स्मृति: अशोक के धम्म में पारिवारिक उत्तरदायित्व को भी नैतिक अनुशासन का हिस्सा माना गया — माता-पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, सेवकों के प्रति करुणा, और पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। • पशुबलि का विरोध: अशोक ने अनावश्यक हिंसा और पशुबलि का विरोध किया। उन्होंने शिकार और पशु वध पर नियंत्रण लगाए तथा पशुओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। धम्म नीति के प्रचार हेतु अशोक ने 'धम्म महामात्र' नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो राज्य के विभिन्न भागों में जाकर धम्म का प्रचार करते थे, प्रजा से संवाद स्थापित करते थे और नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करते थे। धम्म की नीति ने अशोक को न केवल एक धार्मिक नेता के रूप में प्रतिष्ठा दी, बल्कि उन्होंने इसे शासन का भी आधार बनाया। इस नीति ने प्रजा के मन में उनके प्रति आदर और विश्वास पैदा किया और शासन को सेवा का माध्यम बना दिया। अशोक की धम्म नीति आधुनिक लोकतंत्रों के मूल्यों — जैसे धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार, और सामाजिक न्याय — की पूर्वपीठिका कही जा सकती है। इस प्रकार, अशोक का जीवन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है — युद्ध और विस्तार से प्रारंभ होकर करुणा और सेवा में परिवर्तित शासन तक। यह परिवर्तन ही उन्हें विश्व इतिहास का एक विलक्षण, नैतिक और प्रबुद्ध शासक बनाता है। 6. शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से संवाद सम्राट अशोक की नीतियों और कार्यों का प्रभाव केवल उनके शासनकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका दर्शन और प्रशासनिक दृष्टिकोण भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पर दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ गया। अशोक की धम्म नीति, धार्मिक सहिष्णुता और लोककल्याणकारी शासन प्रणाली ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अशोक का सबसे बड़ा समकालीन प्रभाव यह था कि उनके शासनकाल में धार्मिक संघर्ष नगण्य हो गए। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को संरक्षित किया, बल्कि हिंदू, जैन और अन्य पंथों के प्रति भी सम्मान और संरक्षण का भाव बनाए रखा। उनके धम्म लेख इस बात का प्रमाण हैं कि वह केवल बौद्ध सम्राट नहीं थे, बल्कि समावेशी नैतिक शासन के प्रतीक थे। यह परिपक्व धार्मिक दृष्टिकोण एक ऐसे युग में आया जब विश्व के अन्य भागों में धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहे थे। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो अशोक के सिद्धांत और उनके प्रतीक भारत की आधुनिक राष्ट्रीय चेतना में भी अंतर्भूत हो गए। भारत सरकार ने उनके लायन कैपिटल (अशोक स्तंभ, सारनाथ) को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, जो न्याय, शक्ति, करुणा और आत्मसंयम का प्रतीक है। इसी प्रकार भारतीय ध्वज में समाविष्ट अशोक चक्र 24 तीलियों वाला वह चक्र है, जो उनके धम्म के सतत् प्रवाह और कर्मशीलता का बिंब है। यह चक्र केवल एक बौद्ध प्रतीक नहीं, बल्कि समरसता, नैतिकता और सतत विकास का प्रतीक बन गया है। इसके अतिरिक्त, अशोक के वैश्विक बौद्ध प्रचार ने भारत को एशिया में सांस्कृतिक नेतृत्व दिलाया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन और जापान में फैला बौद्ध धर्म आज भी भारत को आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत मानता है। अशोक द्वारा स्थापित यह सांस्कृतिक सेतु न केवल धार्मिक, बल्कि भाषाई, कलात्मक और दार्शनिक रूप से भी भारत की छवि को विस्तृत करता है। राजनीतिक दृष्टि से भी अशोक का ‘राज्य = जनसेवक’ का सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की भावना से मेल खाता है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, संवाद और कल्याण को प्राथमिकता देना — ये सब मूल्य आज की शासन प्रणालियों के लिए अनुकरणीय हैं। 7. प्रशासनिक और सामाजिक सुधार सम्राट अशोक का शासन केवल नैतिकता और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने व्यावहारिक प्रशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में भी अनेक क्रांतिकारी सुधार किए। उनके शासकीय दृष्टिकोण में ‘राजा’ को केवल शासक नहीं, बल्कि प्रजाहितैषी और जनसेवक माना गया। अशोक के प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की विशेषता यह थी कि उनमें नैतिकता और व्यावहारिकता का संतुलित समावेश था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति: अशोक द्वारा किया गया सबसे महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक नवाचार था — ‘धम्म महामात्र’ नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। इन अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था ताकि वे— • धम्म (नैतिक आचरण) के सिद्धांतों का प्रचार कर सकें, • जनसामान्य से संवाद कर उनकी समस्याएं सुन सकें, • विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सहिष्णुता, सौहार्द और संवाद को प्रोत्साहित कर सकें, • और समाज में नैतिक चेतना को विकसित कर सकें। ये महामात्र केवल शासकीय दूत नहीं थे, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद की कड़ी थे, जिन्होंने शासन में उत्तरदायित्व और नैतिकता की भावना को सुदृढ़ किया। लोककल्याणकारी कार्य: अशोक ने शासन को जनसेवा का माध्यम मानते हुए अनेक सामाजिक सुधार आरंभ किए। उनके शासन में किए गए प्रमुख लोककल्याणकारी कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: • चिकित्सा सेवाएं: उन्होंने मानवों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालयों की स्थापना की। शिलालेखों में उल्लेख है कि उन्होंने औषधि, वनस्पतियों और इलाज की सुविधाएं दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँचाने के आदेश दिए। • वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण: मार्गों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए गए ताकि यात्रियों को विश्राम मिल सके। यह न केवल यात्री सुविधा का उपाय था, बल्कि पर्यावरण-संरक्षण की दृष्टि से भी एक अग्रगामी सोच थी। • जल-प्रबंधन: उन्होंने कुओं, जलाशयों और नहरों की खुदाई करवाई ताकि सिंचाई और पीने के पानी की सुविधाएं सुलभ हो सकें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। • सड़कें और विश्राम गृह: व्यापार और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों की मरम्मत करवाई गई और नियमित अंतराल पर ‘धर्मशालाएं’ अथवा विश्राम गृह बनवाए गए। यह उनके शासन की संवेदनशीलता और सुव्यवस्था का परिचायक था। • पशु-संरक्षण और करुणा: अशोक ने पशुबलि को सीमित किया और मांसाहार को हतोत्साहित किया। अनेक शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया और उनके संरक्षण के आदेश जारी किए। प्रशासन की मानवीय दिशा: अशोक ने शासन को एक नैतिक संस्था में रूपांतरित किया, जिसका उद्देश्य केवल कर-संग्रह और सैन्य नियंत्रण नहीं, बल्कि जनहित और नैतिक उत्थान था। उन्होंने न्यायिक सुधारों की दिशा में भी कार्य किया — जैसे कि कैदियों को छूट देना, उनकी सुनवाई में त्वरितता लाना, और दंड प्रक्रिया में करुणा का समावेश करना। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अधिकारी आम जन से सहृदयता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। नारी और समाज: अशोक ने अपने अभिलेखों में स्त्रियों को भी धर्मोपदेश देने और नैतिक आचरण अपनाने की सलाह दी। उनका यह दृष्टिकोण सामाजिक समता और लैंगिक न्याय की दिशा में एक प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। अशोक के प्रशासनिक और सामाजिक सुधार आज के ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की परिकल्पना का प्रारंभिक आदर्श हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शासन की सफलता केवल सैन्य शक्ति या राजस्व संग्रहण में नहीं, बल्कि प्रजा के जीवन को नैतिक, सुरक्षित, और समुन्नत बनाने में है। इस दृष्टि से अशोक का शासन प्राचीन भारत का एक ऐसा युग था, जिसमें राजनीति और नीति का विलक्षण समन्वय दिखाई देता है। 8. बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म केवल एक स्थानीय धार्मिक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि उसने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक संदेशवाहक के रूप में देखा, जिसे सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उनके शासन में पहली बार भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति का प्रयोग करते हुए धर्म और नैतिकता के माध्यम से वैश्विक संवाद की परंपरा की नींव रखी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का स्थापन अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र (महिंदा) और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। श्रीलंका के तत्कालीन राजा देवनंपिय तिस्स के साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को वहाँ केवल एक धार्मिक संदेश के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। महेंद्र और संघमित्रा के प्रभाव से श्रीलंका में बौद्ध धर्म एक स्थायी और प्रभावशाली संस्था बन गया। महाविहार की स्थापना, बोधिवृक्ष का रोपण, और पालि भाषा में धर्मग्रंथों की रचना — यह सब अशोक की प्रेरणा और संरक्षण से संभव हो सका। आज भी श्रीलंका में अशोक को बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। अन्य देशों में प्रचार और कूटनीतिक संबंध अशोक ने केवल श्रीलंका तक ही सीमित न रहकर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सीरिया, मिस्र, यूनान, म्यांमार (बर्मा), थाईलैंड, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचारकों और दूतों को भेजा। उन्होंने इन क्षेत्रों के सम्राटों और शासकों को व्यक्तिगत पत्र और उपदेश भेजे, जिनमें नैतिक शासन, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश निहित था। इन दूतों को ‘धर्म-दूत’ के रूप में जाना गया, जो अशोक के धम्म दर्शन के प्रचारक थे। अशोक की सांस्कृतिक कूटनीति अशोक की यह नीति केवल धर्म-प्रचार की नहीं थी, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और मानवीय कूटनीति थी। उन्होंने इस माध्यम से भारत को विश्व समुदाय में एक नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। यह उस युग के लिए अत्यंत विलक्षण था जब अधिकतर शासक युद्ध और विस्तार में विश्वास रखते थे। अशोक ने “मन जीतने की कूटनीति” (conquest by dharma) अपनाई और इसे ‘धम्म विजय’ कहा। प्रभाव और ऐतिहासिक महत्व • अशोक की इस नीति से बौद्ध धर्म ने एशिया के विभिन्न देशों में गहरी जड़ें जमा लीं। • उन्होंने धार्मिक यात्राओं, बौद्ध विहारों की स्थापना, और पांडुलिपियों के आदान-प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया। • थेरवाद बौद्ध धर्म का विकास और उसका प्रसार मुख्यतः अशोक के प्रयासों का परिणाम है। • भारत ने पहली बार एक ‘वैश्विक सांस्कृतिक राष्ट्र’ की भूमिका निभाई। अशोक का बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार केवल धार्मिक विस्तार नहीं था, बल्कि यह मानवता के नैतिक उत्थान की वैश्विक योजना थी। उन्होंने सत्तावाद की जगह संवाद, विजय की जगह करुणा, और शक्ति की जगह सेवा को महत्व दिया। उनके प्रयासों ने भारत को न केवल एक धार्मिक केंद्र, बल्कि एक नैतिक प्रकाश-स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई, जिसका प्रभाव आज भी बौद्ध देशों की परंपरा और इतिहास में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अशोक का यह योगदान उन्हें भारतीय इतिहास के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत के रूप में स्थापित करता है। 9. आधुनिक भारत में अशोक की प्रासंगिकता सम्राट अशोक, जो लगभग 2300 वर्ष पूर्व भारत पर शासन करते थे, आज भी भारत के राष्ट्रीय जीवन, राजनीतिक दर्शन, और सांस्कृतिक चेतना में गहराई से विद्यमान हैं। स्वतंत्र भारत ने जब अपनी नई पहचान, मूल्य-व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों को गढ़ना शुरू किया, तो अशोक के विचार और प्रतीक स्वाभाविक रूप से इनका आधार बन गए। यह केवल ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा स्थापित नैतिक, धर्मनिरपेक्ष और लोककल्याणकारी मूल्यों को आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव में शामिल करना था। राष्ट्रीय प्रतीकों में अशोक की उपस्थिति भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंहों को बनाया गया। चार मुखों वाले सिंह, जो चारों दिशाओं में न्याय, शक्ति और निर्भीकता का संदेश देते हैं, आज भी भारतीय राज्य की संप्रभुता और नैतिक प्रशासन का प्रतीक हैं। अशोक चक्र, जो 24 तीलियों वाला है और उनके ‘धम्म’ का प्रतीक था, उसे भारतीय तिरंगे के मध्य स्थान दिया गया। यह चक्र सतत गति, धर्म, कर्म और न्याय का प्रतीक बन गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, न्यायालयों, तथा भारतीय मुद्रा और दस्तावेजों पर भी अशोक स्तंभ अंकित किया जाता है, जो शासन की नैतिक और संवेदनशील दिशा की स्मृति कराता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संगति अशोक के शासन में निहित धर्मनिरपेक्षता, लोकसेवा का आदर्श, और प्रजाहितैषिता आज भी भारत के संवैधानिक मूल्य हैं: • उनकी धम्म नीति, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की बात थी, आज के भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल भावना से मेल खाती है। • उन्होंने शासन को जनसेवा का माध्यम माना, और आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का मूल आदर्श — "सत्यमेव जयते" — भी उसी नैतिक नेतृत्व का विस्तार है। • सामाजिक समता, लैंगिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और नैतिक राजनीति जैसे आधुनिक मुद्दों के बीज भी अशोक की नीतियों में दिखाई देते हैं। अशोक की प्रेरणा: समावेशी और नैतिक नेतृत्व का उदाहरण आज जब राजनीति में नैतिक शून्यता, असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन की चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, अशोक का आदर्श मार्गदर्शन का स्रोत बनता है: • उन्होंने दमन नहीं, संवाद को प्राथमिकता दी। • उन्होंने शांति, सह-अस्तित्व, और धम्म विजय की कल्पना को वास्तविकता में बदला। • उन्होंने शासन की भाषा को करुणा और दया में रूपांतरित किया, जो आज की न्यायप्रिय और संवेदनशील प्रशासनिक प्रणाली की नींव है। शिक्षा और युवा चेतना में अशोक आज भारत में इतिहास और नैतिक शिक्षा में अशोक एक प्रेरणास्रोत के रूप में पढ़ाए जाते हैं। उनके जीवन से नैतिक निर्णय-निर्माण, राजनीति में संवेदनशीलता, और सार्वजनिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों की शिक्षा मिलती है। युवाओं के लिए अशोक का जीवन यह दर्शाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप दूसरों की सेवा, करुणा और सत्य में निहित होता है। अशोक की प्रासंगिकता आधुनिक भारत में केवल प्रतीकों या इतिहास की बात नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत नैतिक प्रेरणा है, जो भारत के शासन तंत्र, नागरिक अधिकारों, और लोकतांत्रिक चेतना को दिशा देती है। उनके आदर्श आज भी यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व वह है जो अपने लोगों के प्रति करुणा, उत्तरदायित्व और धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों से प्रेरित हो। इस दृष्टि से अशोक भारतीय सभ्यता के ऐसे प्रकाश-स्तंभ हैं, जिनकी रोशनी आधुनिक लोकतंत्र को भी आलोकित करती है। 10. निष्कर्ष (Conclusion) सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध और सत्ता की परंपरागत व्याख्याओं को नकारते हुए करुणा, नैतिकता और सेवा को शासन का आधार बनाया। उन्होंने ‘धम्म’ के माध्यम से धर्म को केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानवीय संबंधों, सामाजिक कर्तव्यों और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तित कर दिया। अशोक ने सिद्ध किया कि सच्चा शासक वह नहीं जो केवल युद्धों से भूमि जीतता है, बल्कि वह जो जन-मन को जीतकर एक नैतिक समाज की स्थापना करता है। उनका शासन सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण के मूल्यों का आदर्श उदाहरण था। अशोक के विचार और प्रतीक न केवल इतिहास के पृष्ठों में जीवित हैं, बल्कि आधुनिक भारत की आत्मा में भी समाहित हैं। राष्ट्र की चेतना में अशोक का यह योगदान इस बात का प्रमाण है कि एक नैतिक शासक की दृष्टि युगों तक समाज को दिशा दे सकती है। इस प्रकार, सम्राट अशोक का ऐतिहासिक योगदान केवल मौर्य साम्राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने शासन, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे मूल्यों की स्थापना की, जिनका प्रभाव भारत और विश्व दोनों पर आज भी दृष्टिगोचर होता है। अशोक वास्तव में भारत के "धम्म सम्राट" के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। 11. संदर्भ सूची (References) 1. Thapar, Romila. (1997). Ashoka and the Decline of the Mauryas. Oxford University Press. pp. 43–168. 2. Goyal, S. R. (2005). A History of Indian Buddhism. Kusumanjali Prakashan. pp. 213–278. 3. Sharma, R. S. (1983). Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India. Motilal Banarsidass. pp. 201–236. 4. Singh, Upinder. (2008). A History of Ancient and Early Medieval India. Pearson. pp. 320–367. 5. Basham, A. L. (1954). The Wonder That Was India. Rupa Publications. pp. 90–104. 6. Barua, B. M. (1946). Ashoka and His Inscriptions. New Delhi: Government of India Press. 7. Jha, D. N. (2010). Ancient India: In Historical Outline. Manohar Publishers. pp. 134–162. 8. Lahiri, Nayanjot. (2015). Ashoka in Ancient India. Harvard University Press. pp. 178–245. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 7, July 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
Share this

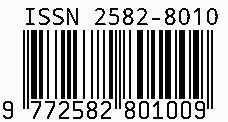
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

