
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 1
January 2026
Indexing Partners
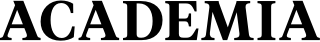




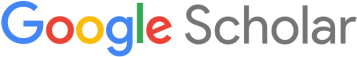








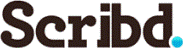




राजस्थान में जलवायु का प्रभाव : एक भौगोलिक विश्लेषण
| Author(s) | पप्पू लाल रैगर |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, अपना विस्तृत क्षेत्रफल, विविध भू-आकृति और सीमांत वातावरण के कारण भारत के उन राज्यों में आता है जो जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के पर्यवेक्षित रुझानों (तापमान, वर्षा, चरम घटनाएँ) और उनके सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अध्ययन में मौसम-स्थानिक मलखिकताओं, कृषि, जल संसाधन, वन एवं पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे पर जलवायु प्रभावों का विवेचन किया गया है। साथ ही, राज्य की अनुकूलन नीतियों विशेषकर राजस्थान राज्य क्रियान्वयन योजना (State Action Plan on Climate Change, SAPCC) और गर्मी-तरंग (Heat Wave) कार्रवाई योजनाओं का आकलन और सुदृढ़ीकरण हेतु मार्गदर्शन भी दिया गया है। मौलिक निष्कर्ष यह हैं कि राजस्थान में औसत तापमान में वृद्धि, न्यूनतम/अधिकतम तापमान चरम का उभार और वर्षा के असममित व अतिव्यापी व्यवहार के प्रमाण उपलब्ध हैं; ये परिवर्तन जल-संकट, उपज में अस्थिरता, चरमराते पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाते हैं। इसलिए समेकित जल प्रबंधन, खेती में अनुकूलन-रचनाएँ, पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय सामूहिक क्षमता निर्माण पर ध्यान आवश्यक है। (मुख्य स्रोत: राजस्थान SAPCC; IMD/वैज्ञानिक अध्ययनों; 1. प्रस्तावना — समस्या का भू-आकृतिक परिप्रेक्ष्य राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.4 प्रतिशत हिस्सा है। इतने विशाल क्षेत्र में जलवायु और भू-आकृतिक विविधता स्वाभाविक है। पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल फैला हुआ है, जहाँ औसत वर्षा मात्र 100-200 मि.मी. प्रतिवर्ष होती है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी जिलों में वर्षा का औसत 600-1000 मि.मी. तक पहुँच जाता है। यही विविधता राजस्थान को जलवायु प्रभावों की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। मरुस्थलीय भागों में रेत के टीलों का विस्तार, शुष्क हवाएँ, उच्च वाष्पन-दर और भूजल की सीमित उपलब्धता जलवायु के असमान प्रभावों को और तीव्र बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर, दक्षिणी अरावली पर्वतमाला के वनक्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक नमीधारक और पर्यावरणीय दृष्टि से स्थिर दिखाई देते हैं। इन दोनों चरम उदाहरणों के बीच अर्ध-शुष्क कृषि क्षेत्र आते हैं, जिनकी निर्भरता मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर है। यही कारण है कि मानसून पैटर्न में कोई भी बदलाव जैसे देर से आगमन, अनियमितता या अल्पावधि में भारी वर्षा कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका पर गहरा प्रभाव डालता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की पारिस्थितिकी अत्यंत नाजुक स्थिति में है। यहाँ का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु में आता है। इसका अर्थ है कि यहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा की तुलना में कहीं अधिक है। भूमिगत जल संसाधनों का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, और कई जिलों में भूजल खारा या अति-दूषित हो चुका है। कृषि, पशुपालन और मानव उपयोग के लिए जल की कमी जलवायु परिवर्तन से और भी गंभीर हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPCC) की रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में तापमान वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति तथा मानसूनी वर्षा की असमानता और अधिक गहराई से महसूस की जाएगी। स्थानीय स्तर पर भी राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में यह स्वीकार किया गया है कि आने वाले दशकों में औसत तापमान में 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभावित है, और वर्षा के पैटर्न में असमानता बढ़ेगी। इसका सीधा असर फसलों की उत्पादकता, पशुधन की सेहत, वनस्पतियों की प्रजातिगत संरचना, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए, राजस्थान की जलवायु समस्या को केवल एक पर्यावरणीय संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक भू-आकृतिक परिप्रेक्ष्य से देखना आवश्यक है। भूगोल हमें यह समझने का अवसर देता है कि किस प्रकार भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृतिक विशेषताएँ और पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित या तीव्र बनाते हैं। उदाहरणस्वरूप, थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर या बाड़मेर जिले का संवेदनशीलता स्तर कोटा या उदयपुर की तुलना में कहीं अधिक है। इसी प्रकार, अरावली पर्वतमाला के वनों का जलवायु शमन में विशेष योगदान है, जबकि रेगिस्तानी जिलों में वनस्पति का लगभग अभाव है। इस संदर्भ में जलवायु के प्रभावों का भौगोलिक विश्लेषण न केवल शैक्षणिक दृष्टि से, बल्कि नीतिगत और विकासात्मक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह विश्लेषण हमें यह समझने में सहायता करता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की अनुकूलन रणनीति अपनाई जानी चाहिए। जैसे मरुस्थल क्षेत्रों में जल-संरक्षण तकनीकों, टपक सिंचाई और मरु-वनस्पतियों के संरक्षण की आवश्यकता है, वहीं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में फसल विविधीकरण और मानसूनी जल के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। निष्कर्षतः, राजस्थान का विशाल क्षेत्रफल, उसकी भौगोलिक विविधता और पारिस्थितिक जटिलताएँ इस राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक विशिष्ट प्रयोगशाला बनाती हैं। जब तक इन प्रभावों का विश्लेषण भू-आकृतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं किया जाएगा, तब तक न तो समस्या की गहराई समझी जा सकेगी और न ही क्षेत्रानुसार उपयुक्त समाधान खोजे जा सकेंगे। 2. अध्ययन के उद्देश्य 1. राजस्थान में मौसम-सम्बंधी परिवर्तन (तापमान, वर्षा और चरम घटनाएँ) के रुझानों का अवलोकन। 2. इन जलवायु परिवर्तनशीलताओं के कृषि, जल संसाधन, पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक ढाँचे पर प्रभाव विश्लेषित करना। 3. संवेदनशीलता और जोखिम-क्षेत्रों (hotspots) की पहचान करना भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र को किन जोखिमों का सामना। 4. राज्य की मौजूदा नीतियों (SAPCC, Heat Action Plans आदि) तथा स्थानीय अनुकूलन उपायों का आकलन करना। 5. नीति-स्तर पर सिफारिशें और क्षेत्रीय/स्थानीय अनुकूलन रणनीतियाँ प्रस्तावित करना। 3. शोध पद्धति (Methodology) इस अध्ययन में राजस्थान की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक (descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (analytical) दोनों है। इसमें न केवल मौजूदा आँकड़ों एवं नीतिगत दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है, बल्कि समयानुसार रुझानों, भौगोलिक क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन और विभिन्न माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त निष्कर्षों का भी एकीकृत मूल्यांकन किया गया है। 3.1 अध्ययन का स्वरूप (Nature of Study) यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों (secondary data) पर आधारित है, किन्तु जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ प्राथमिक स्रोतों जैसे फील्ड रिपोर्ट, आपदा प्रबंधन दस्तावेज और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों का भी उपयोग किया गया है। शोध का केंद्र राजस्थान राज्य है, किंतु विश्लेषण की गहराई बढ़ाने हेतु इसे क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया गया है— 1. पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र (थार मरुस्थल) 2. मध्य राजस्थान का अर्ध-शुष्क क्षेत्र 3. दक्षिणी राजस्थान का वन-आच्छादित एवं आद्र्र जलवायु क्षेत्र यह क्षेत्रीय विभाजन न केवल भौगोलिक विविधता को स्पष्ट करता है बल्कि जलवायु के असमान प्रभावों को भी दर्शाने में सहायक है। 3.2 डाटा स्रोत (Data Sources) शोध के लिए अनेक स्रोतों का समावेश किया गया है, जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है— 1. सरकारी एवं नीतिगत दस्तावेज o Rajasthan State Action Plan on Climate Change (SAPCC) 2022 o विभिन्न जिलों के Heat Wave Action Plan o State Action Plan on Climate Change and Human Health (SAPCCHH) o आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA, NDMA) की वार्षिक रिपोर्टें 2. मौसम विज्ञान एवं ट्रेंड अध्ययन o भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी दीर्घकालीन तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता संबंधी आँकड़े o Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), पुणे द्वारा प्रकाशित अनुसंधान o उपग्रह-आधारित अवलोकन (NOAA, NASA datasets) जिनका उपयोग द्वितीयक साहित्य से किया गया है 3. भौगोलिक विश्लेषण एवं क्षेत्रीय मैपिंग o राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के मानचित्र o Survey of India के टोपोग्राफिकल शीट्स एवं National Remote Sensing Centre (NRSC) से प्राप्त उपग्रह चित्र o GIS आधारित नक्शानिर्माण और क्षेत्रीय विश्लेषण 4. स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित स्रोत o National Health Mission (NHM) एवं Rajasthan Health Department की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्टें o Heat Wave Action Plan में दर्ज स्वास्थ्य प्रभाव o आपदा प्रबंधन से जुड़ी केस-स्टडी (जैसे—2016 हीट वेव, 2019 बाढ़, 2022 सूखा) 5. साहित्य समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन o IPCC AR6 Report (2021–22) o World Bank और UNDP की क्लाइमेट रिपोर्ट o राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित शोध पत्र एवं जर्नल 3.3 शोध की तकनीक (Techniques of Research) अध्ययन में गुणात्मक (qualitative) और परिमाणात्मक (quantitative) दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया गया है— • परिमाणात्मक विश्लेषण: o टाइम सीरीज़ विश्लेषण (1970 से 2022 तक) के आँकड़ों का उपयोग कर तापमान और वर्षा के रुझान का अध्ययन o वर्षानुसार चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता का आँकड़ा-संग्रह o विभिन्न क्षेत्रों में औसत तापमान वृद्धि (°C/दशक) और वर्षा की अनिश्चितता (%) का आकलन • गुणात्मक विश्लेषण: o सरकारी नीतियों और एक्शन प्लान्स की सामग्री का तुलनात्मक विश्लेषण o स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन रिपोर्टों में दर्ज घटनाओं की व्याख्या o क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर जलवायु प्रभाव की व्याख्या 3.4 अध्ययन की सीमा (Limitations of Study) • राजस्थान के सभी जिलों के दीर्घकालिक डेटा समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कुछ स्थानों पर तुलनात्मक अध्ययन सीमित रहा। • उपलब्ध आंकड़े अधिकांशतः district-level aggregates हैं, जिससे ग्राम्य-स्तर पर प्रभावों का सटीक चित्रण कठिन हुआ। • यह अध्ययन केवल जलवायु प्रभावों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है; सामाजिक-राजनीतिक या गवर्नेंस संबंधी आयामों को सीमित रूप में ही शामिल किया गया है। 3.5 शोध प्रक्रिया (Research Process) 1. प्रारंभ में राजस्थान की भौगोलिक एवं जलवायु विविधताओं का अध्ययन किया गया। 2. इसके बाद IMD और SAPCC 2022 से जलवायु परिवर्तन से संबंधित आँकड़े संग्रहीत किए गए। 3. एकत्रित आंकड़ों को GIS एवं सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर की मदद से वर्गीकृत और मैपिंग की गई। 4. क्षेत्रीय विश्लेषण में तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों (पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी राजस्थान) का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। 5. अंततः प्राप्त निष्कर्षों को साहित्य समीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के संदर्भ में पुष्ट किया गया। 4. राजस्थान: जलवायु की भौगोलिक रूपरेखा राजस्थान भारत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे विशाल राज्य है, जो पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं तक विस्तृत है। यह लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसके जलवायु स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु से प्रभावित है, जबकि दक्षिण-पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्से अपेक्षाकृत आर्द्र परिस्थितियों वाले हैं। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु को समझने के लिए इसके भौगोलिक स्वरूप, स्थलाकृति, पवन प्रवाह, वर्षा वितरण, और मौसमी परिवर्तनों का गहन विश्लेषण आवश्यक है। 4.1 स्थलाकृति और जलवायु का संबंध राजस्थान की भौगोलिक रचना विविधतापूर्ण है। राज्य का पश्चिमी भाग विशाल थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहाँ अत्यधिक शुष्कता और कम वर्षा इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। यहाँ रेत के टीलों, विरल वनस्पति और अनियमित वर्षा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी ओर, अरावली पर्वतमाला, जो दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में फैली हुई है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख भौगोलिक इकाई है। अरावली का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त करता है जबकि पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अरावली पर्वत मानसून की हवाओं को रोकने और वर्षा वितरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 4.2 तापमान की चरम सीमाएँ राजस्थान की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता इसके तापमान की चरम सीमाएँ हैं। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45–50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू जैसे मरुस्थलीय जिलों में। वहीं सर्दियों में गंगानगर, सीकर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे भी चला जाता है। तापमान की इस अत्यधिक विविधता के कारण यहाँ जीवन शैली, कृषि पद्धतियों और आर्थिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 4.3 वर्षा वितरण राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 500–600 मिमी के बीच है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता अत्यधिक है। पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर) में वार्षिक वर्षा 100–200 मिमी तक सीमित रहती है, जबकि दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़) में यह 800–1000 मिमी तक पहुँच जाती है। मानसूनी वर्षा राज्य की कुल वर्षा का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करती है, जो सामान्यतः जून से सितंबर के बीच होती है। अनियमित वर्षा और सूखा राजस्थान की प्रमुख जलवायु चुनौतियों में से हैं। 4.4 पवन प्रवाह और आर्द्रता राजस्थान की जलवायु पवन प्रवाह की दिशा और तीव्रता से भी प्रभावित होती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ लू (गर्म और शुष्क हवाएँ) चलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य और कृषि दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में धूल भरी आँधियाँ सामान्य बात हैं। वहीं सर्दियों में ठंडी शुष्क हवाएँ राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करती हैं। आर्द्रता का स्तर भी राजस्थान में क्षेत्रीय रूप से भिन्न है—पश्चिमी भाग में आर्द्रता का स्तर अत्यधिक कम रहता है, जबकि दक्षिण-पूर्वी भाग में यह अपेक्षाकृत अधिक होता है। 4.5 क्षेत्रीय जलवायु विभाजन राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः तीन प्रमुख क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है— 1. पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र: जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू शामिल हैं। यहाँ तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव और अल्प वर्षा प्रमुख विशेषताएँ हैं। 2. अरावली पर्वतीय और मध्यवर्ती क्षेत्र: जिसमें उदयपुर, अजमेर, राजसमंद और जयपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ वर्षा मध्यम है और जलवायु अपेक्षाकृत संतुलित है। 3. दक्षिण-पूर्वी आर्द्र क्षेत्र: जिसमें कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ शामिल हैं। यहाँ वर्षा अधिक होती है और कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। 4.6 जलवायु परिवर्तन और हालिया प्रवृत्तियाँ हाल के वर्षों में राजस्थान की जलवायु पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वर्षा की अनिश्चितता, सूखा और हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि, तथा भूजल स्तर में गिरावट राज्य की प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। तापमान में निरंतर वृद्धि और मानसून के आगमन में देरी जैसी प्रवृत्तियाँ यहाँ की कृषि, जल संसाधन और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु अपनी भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति और पवन प्रवाह के कारण अद्वितीय है, जिसमें शुष्कता, तापमान की चरमता और वर्षा की असमानता इसके मूलभूत लक्षण हैं। यह जलवायु न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी राज्य की पहचान और विकास की दिशा को प्रभावित करती है। 5. पर्यवेक्षित जलवायु रुझान (Observed Trends) राजस्थान की जलवायु संबंधी दशाएँ बीते कुछ दशकों में तीव्र परिवर्तनशीलता और चरम घटनाओं की वृद्धि के रूप में सामने आई हैं। राज्य के भौगोलिक विस्तार और विविधता को देखते हुए यहाँ के जलवायु रुझानों में क्षेत्रीय विषमता (regional heterogeneity) स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD), राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (SAPCC, 2022) तथा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के तापमान, वर्षा, आर्द्रता और चरम जलवायु घटनाओं में उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किए गए हैं। इन रुझानों का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर देखा जा सकता है। 5.1 तापमान रुझान राजस्थान में वार्षिक औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि का संकेत मिलता है। 1951 से 2020 की अवधि में राज्य का औसत सतही तापमान लगभग 0.6–0.8°C तक बढ़ा है। विशेष रूप से, गर्मी के मौसम (मार्च–जून) में अधिकतम तापमान की वृद्धि अधिक स्पष्ट पाई गई है। पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र) में हीट वेव (लू) की आवृत्ति तथा अवधि में वृद्धि हुई है, जिससे गर्मियों में तापजनित रोगों और मृत्यु की घटनाओं का जोखिम भी बढ़ा है। दूसरी ओर, शीत ऋतु (दिसंबर–जनवरी) में न्यूनतम तापमान में गिरावट अपेक्षाकृत कम देखी गई है, जिससे सर्दियों की तीव्रता कुछ क्षेत्रों में घटती प्रतीत होती है। 5.2 वर्षा रुझान राजस्थान का वार्षिक औसत वर्षा स्तर लगभग 500–600 मिमी है, जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) पर निर्भर करता है। 1901–2020 की अवधि में मानसूनी वर्षा में दीर्घकालिक गिरावट की प्रवृत्ति सामने आई है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की असमानता (rainfall variability) और सूखा घटनाओं की आवृत्ति बढ़ी है। वहीं, दक्षिणी राजस्थान (उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर) में कभी-कभी अति-वृष्टि (heavy rainfall events) के मामले बढ़े हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएँ देखने को मिलती हैं। वर्षा वितरण में यह असंतुलन कृषि उत्पादन की स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। 5.3 आर्द्रता और वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) राजस्थान के अधिकांश शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वायु आर्द्रता में कमी और वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि देखी गई है। गर्मी के महीनों में उच्च तापमान और कम आर्द्रता की स्थिति जल संकट को और अधिक गहरा करती है। राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में जलवाष्प दाब (vapour pressure) के स्तर में गिरावट, भूजल के अति-दोहन और सिंचाई जल की आवश्यकता को और बढ़ा देती है। 5.4 चरम जलवायु घटनाएँ (Extreme Events) पिछले कुछ दशकों में राजस्थान में चरम जलवायु घटनाओं (extreme climatic events) की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें प्रमुख हैं: • हीट वेव्स (Heat Waves): पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में हर दशक में इनकी औसत घटनाएँ बढ़ी हैं। • सूखा (Drought): राज्य के पश्चिमी हिस्से में औसतन हर 3–4 वर्षों में सूखा पड़ रहा है, जबकि पहले यह आवृत्ति 5–6 वर्ष की थी। • अति-वृष्टि और बाढ़: दक्षिणी राजस्थान तथा अरावली क्षेत्र में कुछ वर्षों में सामान्य से अधिक वर्षा होने पर फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। • धूल भरी आँधियाँ (Dust Storms): पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में धूल भरी आँधियों की तीव्रता और आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है, जिससे वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़े हैं। 5.5 मौसमी पैटर्न में बदलाव राजस्थान में ऋतु चक्र की समयावधि और मौसमी विशेषताओं में भी बदलाव दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए, मानसून की शुरुआत कभी-कभी देर से होती है, जबकि इसकी वापसी सामान्य से पहले हो जाती है। इसी प्रकार, गर्मी की ऋतु अपेक्षाकृत लंबी खिंच रही है, जबकि शीत ऋतु की अवधि संक्षिप्त होती जा रही है। यह परिवर्तन कृषि चक्रों (cropping cycles) और पारंपरिक जीवनशैली पर सीधा असर डालते हैं। 5.6 क्षेत्रीय विविधताएँ राज्य के भीतर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अलग-अलग रूपों में सामने आते हैं। • थार मरुस्थल: उच्च तापमान, कम वर्षा और लू की घटनाओं में बढ़ोतरी। • अरावली पर्वत क्षेत्र: मानसूनी वर्षा की असमानता और कभी-कभी बाढ़ की स्थितियाँ। • दक्षिणी वन-आच्छादित क्षेत्र: उच्च आर्द्रता, भारी वर्षा और जलजनित आपदाओं की संवेदनशीलता। 6. जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभाव (Geographical Impacts) राजस्थान की भौगोलिक विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अत्यधिक असमान और क्षेत्र-विशेष बनाती है। यहाँ के भिन्न-भिन्न भू-भाग—पश्चिमी थार मरुस्थल, मध्य राजस्थान का अर्ध-शुष्क क्षेत्र, तथा दक्षिणी राजस्थान के वनाच्छादित पर्वतीय इलाके प्रत्येक अपने तरीके से जलवायु के बदलावों को अनुभव कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के ये प्रभाव केवल प्राकृतिक परिदृश्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, जलस्रोतों, जैव विविधता और मानव जीवन पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं। 6.1 थार मरुस्थल और पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे जिले आते हैं, जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर दुष्प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ तापमान में निरंतर वृद्धि और वर्षा में भारी असमानता देखी गई है। मानसून के दौरान वर्षा का एक ही स्थान पर अत्यधिक केंद्रित होना, और शेष समय में लम्बे सूखे का प्रकोप, इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिर रहा है और लवणीयता की समस्या बढ़ रही है। मरुस्थलीकरण की गति तेज हुई है, जिससे खेती योग्य भूमि सिकुड़ रही है। पशुपालन पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है क्योंकि चारागाह घट रहे हैं और पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 9, September 2025 |
| Published On | 2025-09-04 |
Share this

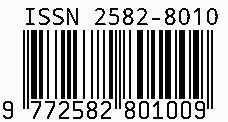
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

