
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 1
January 2026
Indexing Partners
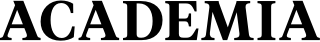




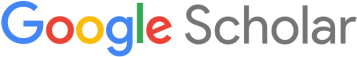








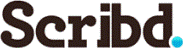




चन्द्रावती (सिरोही) का आठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक व्यापार व वाणिज्य: एक ऐतिहासिक अध्ययन
| Author(s) | SOHAN LAL |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित राजस्थान की भूमि केवल वीरता, स्थापत्य और सांस्कृतिक वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रही, बल्कि इसका व्यापारिक इतिहास भी अत्यंत समृद्ध, गतिशील और बहुआयामी रहा है। इस क्षेत्र ने प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और अनेक नगरों ने यहाँ वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में अपना विकास किया। इन्हीं में एक प्रमुख नाम है — चन्द्रावती, जो वर्तमान में राजस्थान के सिरोही ज़िले में बाणास नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर के रूप में जाना जाता है। चन्द्रावती की स्थापना तथा विकास का काल मुख्यतः आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच रहा, जब भारत के विभिन्न भागों में स्थायी राजवंशों का उदय हो रहा था, और राजनीतिक स्थिरता का प्रभाव सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिलक्षित होने लगा था। यह वह काल था जब परमार और सोलंकी जैसे राजवंशों ने इस क्षेत्र में शासन किया और नगरों के प्रशासन, निर्माण और आर्थिक संरचना को सशक्त रूप प्रदान किया। चन्द्रावती को भी इसी वातावरण में एक सुव्यवस्थित, विकसित और समृद्ध व्यापारिक नगर बनने का अवसर मिला। इस नगर की भौगोलिक स्थिति इसे विशिष्ट बनाती है। यह पश्चिमी भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था, जो गुजरात, मालवा, उत्तरी कोंकण और राजस्थान के अन्य भागों को जोड़ता था। इसके अतिरिक्त, यह नगर बाणास नदी के किनारे स्थित था, जिससे जलस्रोतों की उपलब्धता के कारण कृषि और व्यापारिक गतिविधियाँ सशक्त रूप से संचालित हो पाती थीं। नदी-मार्गों के साथ-साथ थल मार्गों का संगम चन्द्रावती को एक अंतर-क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। इस काल में चन्द्रावती का महत्व केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बहुधार्मिक, सांस्कृतिक और शिल्पपरंपरा से युक्त नगर भी था। यहाँ प्राप्त मूर्तियों, मंदिरों, तोरण द्वारों और स्थापत्य संरचनाओं में न केवल कलात्मक कुशलता परिलक्षित होती है, बल्कि यह दर्शाता है कि नगर में शिल्प उत्पादन और उससे संबंधित वस्तुओं का निर्माण, खपत और निर्यात बड़े पैमाने पर होता था। शैव, वैष्णव और जैन धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ने इस नगर को धार्मिक सहिष्णुता का भी केंद्र बनाया, जिसने व्यापारियों और कारीगरों को एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण प्रदान किया। इस शोध पत्र का उद्देश्य आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य काल में चन्द्रावती की व्यापारिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसमें विशेष रूप से उस समय प्रचलित व्यापारिक मार्गों, प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं, शासकीय प्रोत्साहनों, गिल्ड प्रणालियों (श्रेणियों), बाज़ार व्यवस्था, मुद्रा विनिमय, कर-प्रणाली और व्यापार से जुड़े सामाजिक वर्गों की भूमिका का विवेचन किया गया है। साथ ही, यह भी अध्ययन किया गया है कि तेरहवीं शताब्दी में चन्द्रावती की व्यापारिक गतिविधियों में ह्रास क्यों हुआ — क्या यह केवल राजनीतिक अस्थिरता के कारण था, या इसके पीछे परिवहन मार्गों का परिवर्तन, विदेशी आक्रमण, अथवा आंतरिक आर्थिक असंतुलन जैसे अन्य कारक भी थे। इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि चन्द्रावती केवल स्थापत्य खंडहरों का नगर नहीं था, बल्कि वह अपने समय में एक जीवंत, समृद्ध और प्रभावशाली आर्थिक केंद्र था, जिसकी पहचान आज पुनः शोध और संरक्षण के माध्यम से सामने लाई जा सकती है। इस नगर का व्यापारिक इतिहास न केवल राजस्थान, बल्कि सम्पूर्ण पश्चिम भारत के आर्थिक इतिहास को समझने के लिए एक अनिवार्य आधारशिला सिद्ध हो सकता है। यह शोध-पत्र चन्द्रावती के भूतकालीन व्यापार-वाणिज्य की सामाजिक-आर्थिक परिपक्वता को समझने का एक सशक्त प्रयास है, जो न केवल इतिहासकारों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए भी प्रासंगिक है, जो ऐतिहासिक नगरों के पुनरुत्थान और धरोहर आधारित आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 2. शोध की आवश्यकता और उद्देश्य चन्द्रावती, जो आज सिरोही ज़िले के एक पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचानी जाती है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती थी। इसके भौगोलिक स्थान, स्थापत्य वैभव और धार्मिक विविधता पर कुछ हद तक अनुसंधान हुए हैं, परंतु चन्द्रावती के व्यापार और वाणिज्यिक जीवन पर केंद्रित अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुए हैं। राजस्थान के अन्य व्यापारिक केंद्रों जैसे नागौर, मेड़ता, जैसलमेर या भीनमाल की तुलना में चन्द्रावती के व्यापारिक स्वरूप को इतिहास में वह महत्त्व नहीं मिल पाया है, जो उसे प्राप्त होना चाहिए। शोध की आवश्यकता इस प्रकार स्पष्ट होती है: 1. इतिहास की रिक्तियों की पूर्ति हेतु – चन्द्रावती के व्यापारिक स्वरूप को समझना राजस्थान के आर्थिक इतिहास की उन कड़ियों को जोड़ना है, जो अभी तक अस्पष्ट या अनदेखी रही हैं। यह अध्ययन इस नगर की वाणिज्यिक केंद्रीयता को सामने लाने का कार्य करेगा। 2. पुरातात्विक साक्ष्यों के व्याख्यात्मक उपयोग के लिए – चन्द्रावती से प्राप्त मुद्रा-अवशेष, व्यापारिक गिल्ड शिलालेख, स्थापत्य में प्रयुक्त तकनीकी सामग्री, और मार्ग-संकेतक अवशेष — सभी व्यापारिक गतिविधियों के सशक्त प्रमाण हैं, जिनकी ऐतिहासिक व्याख्या आवश्यक है। 3. समकालीन आर्थिक दृष्टिकोण के निर्माण हेतु – चन्द्रावती के आर्थिक जीवन को समझना, हमें यह जानने में सहायता करता है कि कैसे मध्यकालीन नगर भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक संरक्षण और सामाजिक सहिष्णुता के बल पर एक सफल व्यापारिक इकाई बनते थे। 4. धरोहर संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से – यदि चन्द्रावती की व्यापारिक भूमिका को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उजागर किया जाए, तो इसे एक "व्यापारिक नगर की धरोहर" के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जो शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। शोध के प्रमुख उद्देश्य (Objectives of the Study): • आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य चन्द्रावती के व्यापारिक स्वरूप का ऐतिहासिक अध्ययन करना: इस उद्देश्य के अंतर्गत नगर के व्यापारिक विकास, प्रमुख वस्तुओं, मुद्रा विनिमय, गिल्ड प्रथाओं और बाज़ार संरचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। • व्यापारिक मार्गों, प्रमुख वस्तुओं, तकनीकों और व्यापार से जुड़े सामाजिक वर्गों की पहचान करना: इस बिंदु में प्रमुख भूमि-मार्गों, व्यापारिक कारवाँ, व्यापारी जातियों (जैसे ओसवाल, महाजन, बनिए), तथा स्थानीय कारीगर वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। • चन्द्रावती की आर्थिक समृद्धि में व्यापार की भूमिका का मूल्यांकन करना: शिलालेख, कर प्रणाली, निर्माण कार्य, धार्मिक अनुदानों आदि से यह निर्धारित किया जाएगा कि व्यापार ने स्थानीय शासन और समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। • राजनीतिक परिवर्तनों — जैसे परमारों से सोलंकियों तक शासन और दिल्ली सल्तनत के आक्रमण — का व्यापार पर प्रभाव का विश्लेषण करना: इन घटनाओं के कारण व्यापारिक मार्गों की दिशा, कर-व्यवस्था में परिवर्तन, और व्यापारिक गतिविधियों के ह्रास या परिवर्तन को स्पष्ट किया जाएगा। इस शोध का निष्कर्ष न केवल चन्द्रावती के व्यापारिक स्वरूप को स्पष्ट करेगा, बल्कि यह भी सिद्ध करेगा कि भारत के मध्यकालीन नगर, विशेषकर पश्चिम भारत में, व्यापार केवल आर्थिक क्रिया नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों से गहराई से जुड़ा हुआ एक सामाजिक ढाँचा था। चन्द्रावती उसी ढाँचे का एक विलुप्त किन्तु महत्वपूर्ण स्वरूप है। 3. स्रोत और शोध पद्धति इस अध्ययन में ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। चूँकि चन्द्रावती का व्यापारिक इतिहास एक जटिल सामाजिक-आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ विषय है, अतः शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिससे तथ्यों की प्रमाणिकता और विविधता सुनिश्चित की जा सके। • प्राथमिक स्रोत (Primary Sources): 1. शिलालेख और ताम्रपत्र – चन्द्रावती एवं आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त शिलालेखों में व्यापारिक गिल्डों, दान-पत्रों और कर-मुक्त व्यापार के उल्लेख मिलते हैं। इनसे व्यापारिक संस्थाओं की संरचना, शासकीय नीति और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को समझने में सहायता मिलती है। 2. मुद्रा-अवशेष – विभिन्न कालखंडों की प्रचलित मुद्राओं जैसे परमार, सोलंकी एवं गुजरात के चालुक्य शासकों की मुद्राएँ चन्द्रावती क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इनसे व्यापारिक लेन-देन की सीमा, वस्तु विनिमय की प्रकृति, और आर्थिक समृद्धि का संकेत प्राप्त होता है। 3. उत्खनन रिपोर्ट – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) एवं राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा चन्द्रावती क्षेत्र में किए गए उत्खननों से प्राप्त निर्माण अवशेष, तोरण द्वार, सड़कों के अवशेष, जल संरचनाएँ और शिल्पकला – सभी व्यापारिक गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। 4. विदेशी यात्रियों के विवरण – अल-बरुनी जैसे विद्वान यात्रियों के विवरणों में पश्चिमी भारत के व्यापारिक नगरों की स्थिति का उल्लेख मिलता है, जिससे चन्द्रावती जैसे नगरों की भूमिका का परोक्ष आकलन किया जा सकता है। • द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources): 1. इतिहास ग्रंथ एवं शोध लेख – आधुनिक इतिहासकारों द्वारा रचित ग्रंथ जैसे जे.सी. मेहता की Rajasthan Through the Ages, के.सी. जैन की Ancient Cities and Towns of Rajasthan, तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध प्रबंधों में चन्द्रावती का उल्लेख मिलता है। 2. पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट्स – Indian Archaeology – A Review (IAR) की वार्षिक रिपोर्टों में चन्द्रावती उत्खननों के संक्षिप्त विवरण मिलते हैं जो स्थल की संरचनात्मक पहचान और व्यापारिक संरचनाओं की स्थिति स्पष्ट करते हैं। 3. समकालीन लेखकों की कृतियाँ – समकालीन शिल्प-लेखकों, जैन तीर्थ यात्रियों और स्थानीय इतिहासकारों की कृतियाँ – जैसे प्रबंध चिंतामणि, वंशावली विवरण आदि – से चन्द्रावती के व्यापारिक महत्व और कारीगर वर्ग की जानकारी मिलती है। इस शोध में इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करके एक बहुपरिप्रेक्ष्यीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि चन्द्रावती केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक नगर नहीं, बल्कि एक संगठित, सशक्त और अंतर-क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र था। 4. चन्द्रावती की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक अनुकूलता चन्द्रावती की भौगोलिक स्थिति उसे एक प्राकृतिक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह नगर वर्तमान राजस्थान के सिरोही ज़िले में, बाणास नदी के तट पर, अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित था। यह स्थान गुजरात, मालवा, दक्षिण राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले प्राचीन थल मार्गों तथा जल स्रोतों का मिलन बिंदु था। इससे यह नगर एक महत्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हो पाया। व्यापारिक अनुकूलता के प्रमुख पक्ष: • नदी के निकट होने का लाभ – बाणास नदी, जो चन्द्रावती के निकट प्रवाहित होती है, जल आपूर्ति, कृषि उत्पादन और व्यापारिक वस्तुओं की आवाजाही के लिए अत्यंत अनुकूल थी। नदी किनारे स्थित घाट और जल संरचनाएँ व्यापारिक सामग्री के अस्थायी भंडारण और परिवहन के लिए उपयोगी रही होंगी। • भौगोलिक संगम बिंदु – चन्द्रावती उत्तर-पश्चिम भारत के भीतर एक रणनीतिक स्थिति में स्थित थी। यह मालवा (वर्तमान मध्य प्रदेश), गुजरात (विशेषकर अन्हिलवाड़ा पाटन), और मेवाड़ क्षेत्र को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों पर था। इससे यह नगर व्यापारिक कारवाँओं का स्थायी पड़ाव बन गया। • स्थानीय संसाधनों की प्रचुरता – चन्द्रावती के आस-पास के क्षेत्र में खनिज, पत्थर, धातु, वन-उत्पाद, औषधीय पौधों और कृषि उत्पादन की प्रचुरता थी। इससे यहाँ उत्पादन, विनिमय और निर्यात का एक सशक्त चक्र विकसित हुआ। • आस-पास के धार्मिक केंद्रों से संपर्क – आबू पर्वत, चन्द्रावती के निकट स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल था। यहाँ जैन धर्म के तीर्थ यात्रियों का आगमन होता था, जो चन्द्रावती के बाज़ारों, शिल्पकारों और व्यापारियों के लिए आर्थिक अवसरों का स्रोत बनते थे। • सुरक्षित परिवेश – परमारों और सोलंकियों जैसे शक्तिशाली राजवंशों के संरक्षण में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। इससे व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा बनी रही और व्यापारी वर्ग को आर्थिक आश्वासन मिला। इन समस्त तत्वों के समन्वय से चन्द्रावती मध्यकालीन राजस्थान का एक प्रमुख व्यापारिक नगर बन सका, जिसकी आर्थिक समृद्धि, स्थापत्य वैभव और शिल्प-उत्पादन इसकी भौगोलिक विशेषताओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था। इस स्थिति ने चन्द्रावती को केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय व्यापारिक नेटवर्क का एक अनिवार्य भाग बना दिया। 5. प्रमुख व्यापारिक वस्तुएँ और उत्पादन आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य चन्द्रावती एक समृद्ध व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ, जिसकी आर्थिक धुरी वस्तु-निर्माण, कारीगरी, कृषि उत्पाद और औषधीय वनस्पतियों पर आधारित थी। यह नगर केवल उपभोग नहीं, बल्कि उत्पादन और निर्यात का भी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था। चन्द्रावती से उत्पादित वस्तुएँ राजस्थान, गुजरात, मालवा और उत्तर भारत के अन्य भागों तक पहुँचती थीं। इन व्यापारिक वस्तुओं की विविधता यह दर्शाती है कि नगर में बहुस्तरीय आर्थिक गतिविधियाँ चलती थीं, जो विभिन्न जातियों, श्रेणियों और सामाजिक वर्गों से जुड़ी हुई थीं। मुख्य व्यापारिक वस्तुएँ एवं उत्पादन क्षेत्र: • धातु उद्योग: चन्द्रावती क्षेत्र में तांबा, कांसा, लोहे और चाँदी का कार्य प्रचलित था। यहाँ हथियार, औज़ार, पूजा सामग्री, बर्तन और आभूषण तैयार किए जाते थे। खुदाई में प्राप्त लोहे के औज़ार और तांबे के सिक्के इस उद्योग के सशक्त प्रमाण हैं। इन धातुओं से बनी वस्तुएँ आस-पास के कृषि क्षेत्रों तथा तीर्थ स्थलों पर भी भेजी जाती थीं। • मूर्तिकला एवं शिल्पकला: चन्द्रावती की मूर्तिकला अपनी उच्च गुणवत्ता, विषय विविधता और कलात्मक finesse के लिए प्रसिद्ध थी। विशेष रूप से विष्णु, महिषासुरमर्दिनी, शिव-पार्वती, गणेश, जैन तीर्थंकरों और स्थानीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ बनाई जाती थीं। इन मूर्तियों का व्यापार धार्मिक स्थलों, मंदिरों, तथा स्थानीय एवं बाहरी व्यापारियों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक होता था। • कृषि उत्पाद: बाणास नदी के कारण उपजाऊ भूमि के क्षेत्र में अनाज, चना, गेहूँ, तिलहन और मसालों की खेती होती थी। दलहन और मसाले मालवा और गुजरात जैसे क्षेत्रों में व्यापार के लिए भेजे जाते थे। यह नगर कृषि-आधारित उत्पादों के भंडारण और वितरण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। • कपड़ा उद्योग और रंगाई: वस्त्र निर्माण और प्राकृतिक रंगों से रंगाई, विशेष रूप से बूटेदार कपड़े, रेशमी थान, सूती वस्त्र आदि, चन्द्रावती के हस्तकला उद्योग का प्रमुख हिस्सा थे। यहाँ के कपड़े स्थानीय उपभोग के साथ-साथ व्यापार के माध्यम से बाहर भी भेजे जाते थे। कुछ विशेष प्रकार की रंगाई तकनीकें क्षेत्रीय विशिष्टता रखती थीं। • गंधद्रव्य एवं औषधियाँ: अरावली क्षेत्र के वनों से प्राप्त गंधक, कपूर, अगर, चंदन, तुलसी, आंवला, नीम और अन्य औषधीय पौधों से निर्मित औषधियाँ और इत्र स्थानीय चिकित्सकों (वैद्यों) द्वारा निर्मित होकर व्यापार में प्रयुक्त होती थीं। यह वस्तुएँ गुजरात के समुद्री व्यापारियों के माध्यम से अरब और फारस तक पहुँचती थीं। • पत्थर एवं निर्माण सामग्री: चन्द्रावती से पास की पहाड़ियों से प्राप्त बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर जैसे पत्थरों का उपयोग न केवल स्थानीय निर्माण में हुआ, बल्कि मंदिर निर्माण और मूर्तिकला के लिए यह सामग्री अन्य क्षेत्रों को भी निर्यात की जाती थी। इन वस्तुओं के व्यापार ने चन्द्रावती को केवल एक उपभोक्ता नगर नहीं, बल्कि एक सृजनशील वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। 6. व्यापारिक संरचना और संगठन चन्द्रावती में व्यापारिक जीवन केवल वस्तु विनिमय तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक संगठित, संरचित और सामाजिक रूप से समायोजित प्रणाली का उदाहरण था। नगर में व्यापार से जुड़ी संस्थाएँ, श्रेणियाँ, कर संरचनाएँ, तथा सामाजिक परिपाटियाँ कार्यरत थीं, जो व्यापारिक व्यवस्था को स्थायित्व और अनुशासन प्रदान करती थीं। मुख्य घटक: • स्थानिक बाज़ार और मंडियाँ: चन्द्रावती में साप्ताहिक हाट-बाज़ार और स्थायी मंडियाँ स्थापित थीं। नगर के मध्य में 'राजकीय बाज़ार' तथा मंदिरों के निकट 'धार्मिक बाज़ार' चलाए जाते थे, जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ नियमित रूप से होती थीं। ये मंडियाँ व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक आदान-प्रदान का भी केंद्र थीं। • श्रेणियाँ (Guilds) और समितियाँ: व्यापारियों और कारीगरों के संगठन – जिन्हें श्रेणियाँ या निगम कहा जाता था – स्थानीय स्तर पर अत्यंत शक्तिशाली संस्थाएँ थीं। ये श्रेणियाँ व्यापार की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण, विवाद समाधान, और सामूहिक सुरक्षा जैसे विषयों पर कार्य करती थीं। कई शिलालेखों में 'श्रेणिप्रमुख' का उल्लेख मिलता है जो इन समितियों के मुखिया होते थे। • कर व्यवस्था और चुंगी प्रणाली: व्यापारिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे जैसे – नगर प्रवेश कर (द्वारकर), मार्ग कर (सेतुकर), बिक्री कर और व्यापार अनुज्ञा कर (व्यवसायिक अनुमति)। शासक वर्ग ने कभी-कभी प्रतिष्ठित व्यापारिक श्रेणियों को कर में छूट दी, जिससे उनकी साख और गतिविधियाँ बढ़ीं। चुंगी चौकियाँ नगर की सीमाओं पर स्थित थीं। • लेखांकन और मुद्रा विनिमय प्रणाली: व्यापार में लेखन प्रणाली का उपयोग भी होता था। नगर के व्यापारियों के पास व्यक्तिगत मुंशी या कायस्थ होते थे, जो लेखा-जोखा रखते थे। व्यापार में धातु-मुद्राएँ प्रयोग में लाई जाती थीं, और ताम्र पत्रों पर लेन-देन के प्रमाण मिलते हैं। यह समूची व्यापारिक संरचना यह दर्शाती है कि चन्द्रावती का व्यापार न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक व्यापक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता था। 7. शासकीय संरक्षण और विदेशी संपर्क चन्द्रावती की व्यापारिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था — स्थानीय राजाओं द्वारा दिया गया संरक्षण। परमार और सोलंकी शासकों ने व्यापार को केवल आर्थिक गतिविधि न मानकर इसे राज्य के वैभव और सामाजिक स्थायित्व का आधार माना। • सड़क एवं परिवहन व्यवस्था: राजकीय मार्गों की सुरक्षा के लिए सैनिक टुकड़ियाँ तैनात की जाती थीं। सड़कों की मरम्मत, धर्मशालाओं का निर्माण, और जल संरचनाओं की उपलब्धता व्यापारिक यात्राओं को सुगम बनाती थी। • करों में रियायतें: विशिष्ट व्यापारिक समुदायों और गिल्डों को करों में छूट प्रदान की जाती थी, विशेषकर धार्मिक आयोजन या समाजोपयोगी दान करने वाले व्यापारियों को विशेष सम्मान भी प्राप्त होता था। • मुद्रा नियंत्रण और सिक्के जारी करना: परमारों और सोलंकियों द्वारा जारी मुद्राएँ व्यापारिक लेन-देन के लिए एक स्थिर और स्वीकार्य माध्यम बनीं। इससे व्यापारिक व्यवस्था में एकरूपता आई। • विदेशी संपर्क और पारमार्थिक संवाद: पश्चिमी एशिया, फारस और अरब देशों से आने वाले व्यापारिक कारवाँ कभी-कभी गुजरात के बंदरगाहों से चन्द्रावती के भीतर व्यापार करते थे। अल-बरुनी जैसे यात्रियों ने चन्द्रावती जैसे नगरों के व्यापारिक वैभव का संकेत अपने ग्रंथों में दिया है। राजशक्ति और व्यापार का यह सहयोग चन्द्रावती को एक राज-समर्थित वाणिज्यिक केंद्र बनाता है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति संभव हुई। 8. व्यापार का पतन और आर्थिक प्रभाव तेरहवीं शताब्दी आते-आते चन्द्रावती की व्यापारिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट आने लगी। यह पतन आकस्मिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया कार्यरत थी। प्रमुख कारण: • दिल्ली सल्तनत के आक्रमण: तुर्क आक्रमणों के दौरान चन्द्रावती की भौगोलिक स्थिति उसे सैन्य संघर्षों के बीच ला खड़ा करती है। इस दौरान नगर को विध्वस्त किया गया, जिससे न केवल शासकीय ढांचा टूटा बल्कि व्यापारिक संरचना भी ध्वस्त हुई। • राजनीतिक संरक्षण का अभाव: स्थानीय राजवंशों की पराजय और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण व्यापारी वर्ग असुरक्षित महसूस करने लगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों का प्रवाह बाधित हुआ। • व्यापार मार्गों में बदलाव: दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ व्यापारिक मार्गों की दिशा दिल्ली और नई राजधानी केंद्रों की ओर स्थानांतरित होने लगी, जिससे चन्द्रावती जैसे पुराने नगर अप्रासंगिक होने लगे। • नए व्यापारिक केंद्रों का उदय: जालौर, भीनमाल, अहमदाबाद जैसे नगर नए व्यापारिक केंद्र बनकर उभरे, जिससे चन्द्रावती के महत्व में ह्रास हुआ। इस प्रकार, चन्द्रावती की आर्थिक गिरावट का प्रभाव न केवल नगर पर पड़ा, बल्कि आसपास के कारीगरों, किसानों, व्यापारियों और धार्मिक संस्थानों के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। एक समृद्ध वाणिज्यिक केंद्र इतिहास के गर्त में समा गया, और आज केवल उसके अवशेष ही हमारी चेतना में शेष रह गए हैं। 9. निष्कर्ष चन्द्रावती, सिरोही ज़िले की गोद में बसा एक ऐसा ऐतिहासिक नगर रहा है, जो न केवल स्थापत्य और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य भारत के व्यापारिक भूगोल में भी एक विशिष्ट स्थान रखता था। बाणास नदी के तट पर स्थित इस नगर ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधन-संपन्नता, राजकीय संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता और शिल्प-कौशल की परंपरा के बल पर एक सशक्त वाणिज्यिक केंद्र के रूप में पहचान बनाई। चन्द्रावती का व्यापार केवल वस्त्र, धातु, मूर्तिकला या कृषि उत्पाद तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ की श्रेणियाँ, गिल्ड प्रणाली, कर व्यवस्था और व्यापारी समुदायों ने इसे संगठित वाणिज्य का आदर्श उदाहरण बनाया। यह नगर केवल माल के लेन-देन का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक अंतर्संबंधों का जीवंत केंद्र था, जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ नगर की सांस्कृतिक गतिशीलता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थीं। परंतु तेरहवीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत का प्रसार हुआ, तो चन्द्रावती की यह समृद्धि राजनीतिक अस्थिरता, आक्रमणों और संरचनात्मक पतन के साथ बिखरने लगी। यह नगर, जो कभी व्यापारिक मार्गों का संगम था, धीरे-धीरे ऐतिहासिक स्मृति में विलीन होता गया। इसके अवशेष आज भले ही खंडहरों के रूप में उपस्थित हों, परंतु वे उस सुनहरे अतीत की मौन गवाही देते हैं, जिसमें चन्द्रावती ने राजस्थान के मध्यकालीन व्यापार को दिशा और स्थायित्व प्रदान किया। इस शोध का निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि चन्द्रावती जैसे नगरों का व्यापारिक इतिहास केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी विश्लेषणीय है। यहाँ की वाणिज्यिक परंपराएँ, बाजार संरचनाएँ, गिल्डें, सामाजिक-सांस्कृतिक संतुलन – सभी यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में व्यापार केवल जीविकोपार्जन नहीं, बल्कि जीवन की विविध परतों का केंद्र बिंदु रहा है। आज जब हम धरोहर संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन की बात करते हैं, तो चन्द्रावती जैसे नगरों का अध्ययन न केवल अतीत की समझ के लिए उपयोगी है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरक है। ऐसे नगरों को केवल ऐतिहासिक curiosity न मानकर, शोध, पुनरुत्थान और संरक्षण के योग्य सांस्कृतिक पूँजी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि चन्द्रावती के व्यापारिक इतिहास को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, पुरातात्विक योजनाओं और सांस्कृतिक नीति-निर्माण में उचित स्थान दिया जाए, ताकि यह अदृश्य हो रही धरोहर, फिर से हमारी सामूहिक चेतना में प्रतिष्ठित हो सके। 10. संदर्भ सूची (References) 1. Jaina, H.L. (1972). Ancient Cities and Towns of Rajasthan. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 112–130. 2. Mehta, J.C. (1980). Rajasthan Through the Ages: Trade and Commerce. Jaipur: Rajasthan State Archives. pp. 45–62. 3. Jain, Kailash Chand. (1975). Trade and Traders in Western India (AD 1000–1300). Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan. pp. 89–106. 4. Sharma, Dasharatha. (1966). Early Chauhān Dynasties. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 171–190. 5. Indian Archaeological Survey (ASI). (1987–2005). Indian Archaeology – A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India. Relevant Volumes. pp. 221–239. 6. Mishra, K.C. (1994). Guilds in Ancient India. Varanasi: Chowkhamba Vidya Bhavan. pp. 62–77. 7. Tripathi, R.S. (1960). History of Ancient India. Allahabad: Central Book Depot. pp. 343–356. 8. Al-Biruni (trans. Sachau, E.C.). (1910). Alberuni’s India. London: Kegan Paul. pp. 188–191. 9. Rajasthan State Archives, Bikaner. (2003). Documents on Medieval Trade Routes in Western India. Unpublished archival manuscripts and maps. 10. Chandra, Satish. (2000). Medieval India: From Sultanat to the Mughals (1200–1526). New Delhi: Har-Anand Publications. pp. 47–56. 11. Jain, Nirmal Kumar. (2008). Chandravati: An Archaeological and Historical Perspective. Jaipur: Rajasthan Puratattva Academy. pp. 15–49. 12. Gupta, Parmeshwari Lal. (1969). Coins. New Delhi: National Book Trust. pp. 102–118. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 7, July 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
Share this

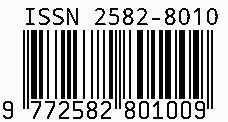
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

