
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 1
January 2026
Indexing Partners
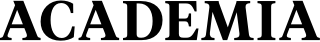




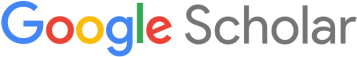








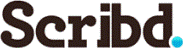




राजस्थान में जल संसाधनों की स्थिति और प्रबंधन रणनीतियों का विश्लेषण: एक भौगोलिक दृष्टिकोण
| Author(s) | Shipra Vyas |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, भारत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद, प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर जल संसाधनों के संदर्भ में अत्यंत संकटग्रस्त है। इसकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु संरचना और भू-आकृतिक विशेषताएँ इसे एक अर्ध-शुष्क से लेकर पूर्णतः शुष्क प्रदेश में परिवर्तित करती हैं। राज्य का लगभग 60% क्षेत्रफल थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहाँ तापमान की अत्यधिक परिवर्तनशीलता, अनियमित एवं न्यून वर्षा, और उच्च वाष्पीकरण दर के कारण जल की उपलब्धता न केवल सीमित है, बल्कि उसका पुनर्भरण भी कठिन होता जा रहा है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 500 मिमी से भी कम है, और वह भी अत्यंत असमान रूप से वितरित होती है—पूर्वी जिलों में अपेक्षाकृत अधिक तथा पश्चिमी भागों में अत्यल्प। इस असंतुलन के कारण राज्य में "जल की भौगोलिक विषमता" (geographical disparity of water) एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। अनेक जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में भूजल स्तर गंभीर रूप से नीचे जा चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव ने सतही जल स्रोतों को भी संकटग्रस्त बना दिया है। इस परिस्थिति को और अधिक जटिल बनाती है राज्य की बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि क्षेत्र की जल पर अत्यधिक निर्भरता। जल उपयोग की वर्तमान प्रवृत्तियाँ न तो सतत हैं और न ही समानुपातिक। एक ओर जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक उपायों का समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। जल की इस विकट स्थिति में राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएँ और स्थानीय समुदाय अपने-अपने स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रयास कर रहे हैं। कुछ जिलों में पारंपरिक जल संरचनाओं जैसे बावड़ियों, टांकों और जोहड़ों के पुनर्जीवन के उदाहरण उत्साहवर्धक हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीकी नवाचारों जैसे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, ड्रिप सिंचाई, और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसी रणनीतियाँ भी अपनाई जा रही हैं। यह शोध पत्र राजस्थान में जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का भौगोलिक विश्लेषण करता है, जिसमें जल स्रोतों की प्रकार, वितरण, गुणवत्ता और उपयोग की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही, यह शोध जल संकट के कारणों को स्पष्ट करने के साथ-साथ उन प्रबंधन रणनीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा भी करता है जो राज्य में जल संरक्षण, पुनर्भरण और वितरण को संतुलित एवं सतत बनाने के लिए प्रयुक्त की जा रही हैं। राजस्थान की जल स्थिति को केवल एक पर्यावरणीय संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। इस चुनौती का समाधान केवल तकनीकी उपायों से नहीं, बल्कि स्थानीय सहभागिता, पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों के एकीकृत प्रयोग से ही संभव हो सकता है। इसलिए, इस शोध का उद्देश्य जल संसाधनों के बहुआयामी स्वरूप को समझते हुए, एक समावेशी और व्यवहारिक जल प्रबंधन नीति की आवश्यकता को रेखांकित करना है। 2. शोध की आवश्यकता (Need of the Study) राजस्थान, जहाँ जल को जीवन का पर्याय माना जाता है, आज स्वयं एक गहन जल संकट का सामना कर रहा है। राज्य की पारिस्थितिक और आर्थिक संरचना जल पर अत्यधिक निर्भर है, किंतु यहाँ जल की उपलब्धता प्राकृतिक रूप से अत्यंत सीमित है। इस सीमितता के बीच, बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने जल की मांग को अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो गया है। जल की यह कमी केवल फसलों की सिंचाई या पीने के पानी की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राज्य के सामाजिक-आर्थिक तानेबाने पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। उदाहरण के लिए, अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जल के अभाव के कारण पशुपालन और कृषि रोजगार संकट में आ गए हैं, जिससे पलायन की समस्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधनों की असमान भौगोलिक उपलब्धता ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास असंतुलन को भी बढ़ावा दिया है। जल संकट से उत्पन्न समस्याएँ केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थायित्व और पारिस्थितिकीय संतुलन से भी जुड़ी हैं। यह संकट जलवायु परिवर्तन की वैश्विक प्रक्रिया से भी प्रभावित हो रहा है, जिससे वर्षा की अनिश्चितता और वाष्पीकरण दर में वृद्धि हो रही है। ऐसे में, राजस्थान के लिए एक ऐसी जल नीति और प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता है, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध हो, बल्कि स्थानीय समाज की आवश्यकताओं, पारंपरिक ज्ञान और भौगोलिक विविधताओं के साथ तालमेल भी स्थापित कर सके। इस शोध की आवश्यकता इसलिए भी प्रबल है क्योंकि अब तक जल संसाधनों पर केंद्रित अधिकांश अध्ययनों में या तो केवल तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं या वे क्षेत्रीय विविधताओं को अनदेखा करते रहे हैं। एक समग्र और भूगोलिक परिप्रेक्ष्य से किया गया अध्ययन राज्य की विविध जल समस्याओं और उनके संभावित समाधानों को बेहतर तरीके से उजागर कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में जल प्रबंधन की मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी इस शोध का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान में चल रही योजनाएँ जैसे ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान’, ‘जल जीवन मिशन’ आदि कितनी व्यवहारिक सिद्ध हो रही हैं और इनकी पहुँच एवं क्रियान्वयन में क्या बाधाएँ हैं। इस प्रकार, यह शोध न केवल राजस्थान में जल संसाधनों की स्थिति को उजागर करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार की रणनीतियाँ, नीतियाँ और सामुदायिक सहभागिता इस संकट को अवसर में बदल सकती हैं। जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि यह राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक जीवनरेखा है — और यही तथ्य इस अध्ययन को अत्यंत आवश्यक, प्रासंगिक और समयोचित बनाता है। 3. उद्देश्य (Objectives) इस शोध का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में जल संसाधनों की स्थिति को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझना एवं जल प्रबंधन के व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं: 1. राजस्थान राज्य में जल संसाधनों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन करना, जिसमें उनका वितरण, प्रकार और उपलब्धता शामिल हो। 2. राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के प्रमुख स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलें, और भूजल की उपयोगिता, गुणवत्ता तथा क्षेत्रीय महत्व का विश्लेषण करना। 3. जल संकट उत्पन्न होने के प्रमुख प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों की पहचान करना और उनका विवेचन करना। 4. वर्तमान में राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा समुदायों द्वारा अपनाई जा रही जल प्रबंधन रणनीतियों का मूल्यांकन करना, उनकी प्रभावशीलता को परखना। 5. जल संरक्षण एवं उसके सतत उपयोग हेतु व्यवहारिक, सुलभ और भूगोल-आधारित समाधान एवं सुझाव प्रस्तावित करना, जो राज्य की भौगोलिक विविधताओं के अनुरूप हों। 4. अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएँ (Geographical Features of the Study Area) राजस्थान भारत का पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र घेरता हुआ एक विशाल भूभाग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य भौगोलिक रूप से अत्यंत विविध है, जहाँ की जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति और संसाधन वितरण में तीव्र विषमता देखने को मिलती है। राज्य का लगभग 70% क्षेत्रफल शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा मात्र 500 मिमी के आसपास है। यह वर्षा भी भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत असमान रूप से वितरित होती है—पूर्वी राजस्थान में यह अपेक्षाकृत अधिक (700–1000 मिमी) है, जबकि पश्चिमी भागों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि में यह 100–200 मिमी तक सीमित रह जाती है। राज्य को भौगोलिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला दो भागों में बाँटती है—पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली की यह प्राचीन श्रृंखला जलवायु और जल निकासी के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। पर्वतमालाएँ जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, जिससे नदियों का बहाव दिशा और जलग्रहण क्षेत्र प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में रेत के टीलों, शुष्क पठारों, नमक की झीलों, तथा छिछले बेसिनों की भू-आकृति जल संचयन और प्रवाह को नियंत्रित करती है। इन भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना जल संसाधनों की वास्तविक स्थिति और प्रबंधन रणनीतियाँ न तो समझी जा सकती हैं और न ही प्रभावी रूप से लागू की जा सकती हैं। 5. जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति (Present Status of Water Resources in Rajasthan) राजस्थान में जल संसाधनों की स्थिति अत्यंत जटिल और असंतुलित है। राज्य में सतही जल स्रोतों की कमी और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता ने जल संकट को गहरा कर दिया है। जल संसाधनों को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है—नदियाँ, झीलें और भूजल। 5.1 नदियाँ (Rivers) राजस्थान की नदियों में अधिकांश मौसमी (seasonal) प्रवाह वाली हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में ही जल प्रवाह देखा जाता है। राज्य में केवल एक प्रमुख नदी चंबल ही बारहमासी (perennial) है। • चंबल नदी: यह यमुना की सहायक नदी है और राज्य के दक्षिण-पूर्वी जिलों जैसे कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में बहती है। यह नदी राजस्थान में सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन दोनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। • बनास नदी: यह एक मौसमी नदी है जो अरावली की पर्वतमालाओं से निकलकर मेवाड़ क्षेत्र से गुजरती है और कृषि हेतु मुख्य जल स्रोतों में से एक है। • लूनी नदी: यह पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है, जिसका जल खारा होता है। यह नदी बाड़मेर और जोधपुर जिलों से बहती है और मरुस्थलीय जल निकासी तंत्र का हिस्सा है। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ जलग्रहण क्षमता में सीमित और मौसमी प्रवाह की होती हैं, जिससे सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती। 5.2 झीलें (Lakes) राजस्थान झीलों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से उदयपुर, जिसे "झीलों की नगरी" कहा जाता है। अधिकांश झीलें मानव निर्मित (artificial) हैं, जिनका निर्माण वर्षा जल संचयन एवं शहरी जलापूर्ति हेतु किया गया था। • पुष्कर झील (अजमेर): यह एक धार्मिक और पारंपरिक महत्व की झील है, जो स्थानीय जलवायु और धार्मिक पर्यटन दोनों को प्रभावित करती है। • पिछोला एवं फतेहसागर (उदयपुर): ये झीलें उदयपुर की जलापूर्ति, पर्यटन और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सम्भर झील: यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी जल की झील है, जहाँ से औद्योगिक नमक का उत्पादन किया जाता है। यह झील पारिस्थितिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए। इन झीलों की पारिस्थितिकीय स्थिति हाल के दशकों में प्रदूषण, शहरीकरण और अवैध अतिक्रमण के कारण कमजोर हुई है। 5.3 भूजल (Groundwater) राजस्थान की जल आपूर्ति प्रणाली में भूजल का लगभग 90% योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कृषि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए भूजल ही एकमात्र स्रोत है। परंतु इसकी स्थिति दिन-प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। • अनेक जिलों जैसे नागौर, बीकानेर, बाड़मेर आदि में भूजल स्तर 100 मीटर से अधिक नीचे चला गया है। • जल गुणवत्ता भी एक गंभीर समस्या बन गई है। कई क्षेत्रों में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, और खारापन की अधिकता देखी गई है, जो स्वास्थ्य और कृषि दोनों के लिए हानिकारक है। भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा जल संचयन की उपेक्षा, और पुनर्भरण की अनुपस्थिति ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। 6. जल संकट के प्रमुख कारण (Major Causes of Water Crisis in Rajasthan) राजस्थान में जल संकट एक बहुआयामी समस्या है, जिसके पीछे प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत कारण समाहित हैं। इस संकट की जड़ें केवल वर्षा की कमी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके लिए अनेक अंतर्संबंधित कारक उत्तरदायी हैं। 1. असमान और अनिश्चित वर्षा: राजस्थान में वर्षा न केवल अल्प मात्रा में होती है, बल्कि उसका वितरण भी अत्यंत असमान होता है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 500 मिमी के आसपास है, लेकिन यह भी निश्चित नहीं है। कई वर्षों तक लगातार सूखे की स्थिति बन जाती है, जिससे भूजल पुनर्भरण बाधित होता है और मौसमी नदियाँ, झीलें व टांके समय पर भर नहीं पाते। वर्षा की अनियमितता के कारण जल संग्रहण की योजना बनाना भी कठिन हो जाता है। 2. भूजल का अत्यधिक दोहन: राज्य की 90% से अधिक जल आवश्यकताएँ भूजल पर निर्भर हैं। आधुनिक पंप तकनीकों और विद्युत सब्सिडी ने भूजल दोहन को तीव्र बना दिया है। अनियंत्रित ट्यूबवेल और बोरवेल ने प्राकृतिक पुनर्भरण की दर से कहीं अधिक पानी निकाल लिया है, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर 100 मीटर से भी अधिक नीचे चला गया है। इसका सीधा असर कृषि उत्पादन, पीने के पानी की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता पर पड़ा है। 3. वृक्षावरण की कमी: वनस्पति आवरण जल संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु राजस्थान में पिछले कुछ दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई और शहरी विस्तार ने वनों के क्षेत्रफल को सीमित कर दिया है। परिणामस्वरूप वर्षा जल का भूमि में अवशोषण और जलग्रहण क्षमता घट गई है, जिससे भूजल पुनर्भरण में कमी आई है। 4. मरुस्थलीकरण (Desertification): थार मरुस्थल का क्षेत्र धीरे-धीरे विस्तृत होता जा रहा है, जो जल स्रोतों को रेतीले टीलों से ढक देता है। भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण बढ़ जाता है और पारंपरिक जल संरचनाएँ बेकार हो जाती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे जिलों में यह स्थिति अधिक गंभीर है। 5. जल प्रबंधन में नीतिगत कमी: राज्य में जल प्रबंधन को लेकर दीर्घकालिक, समन्वित और व्यवहारिक नीति की कमी देखी गई है। पारंपरिक जल प्रणालियों जैसे जोहड़, नाड़ी, टांके आदि को उपेक्षित कर आधुनिक संरचनाओं पर अत्यधिक निर्भरता ने समस्या को बढ़ाया है। कई जल संरचनाओं का रखरखाव नहीं हो पाता, जिससे वे अनुपयोगी हो जाते हैं। इसके अलावा, जल उपयोग में अनुशासनहीनता, अनुपयुक्त सिंचाई तकनीकों और जन जागरूकता की कमी भी संकट को गहराती है। 7. जल प्रबंधन रणनीतियाँ (Water Management Strategies in Rajasthan) राजस्थान सरकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जल संकट से निपटने के लिए अनेक रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। इनमें पारंपरिक उपायों का पुनरुद्धार, नवीन तकनीकों का समावेश और जनसहभागिता को प्राथमिकता दी गई है। 7.1 पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार राजस्थान की जल संस्कृति सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक संरचनाओं पर आधारित रही है। • बावड़ियाँ, जोहड़, नाड़ी, टांके जैसे जल संरचनाएँ कभी ग्रामीण जीवन की रीढ़ हुआ करती थीं। अब पुनः इनका संरक्षण और पुनरुद्धार किया जा रहा है। • स्वयंसेवी संस्थाओं और NGOs के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जल संग्रहण साधनों को सक्रिय किया गया है। उदाहरण के लिए, अलवर जिले में तरुण भारत संघ द्वारा जोहड़ और चेक डैम बनाकर भूजल स्तर में वृद्धि की गई है। 7.2 जल नीतियाँ और योजनाएँ राजस्थान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया जा रहा है: • मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA): वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण हेतु ग्राम पंचायतों को सक्रिय भूमिका दी गई है। • जल जीवन मिशन: केंद्र सरकार की यह योजना हर घर तक नल से जल पहुँचाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें राजस्थान भी अग्रसर है। • राजस्थान जल नीति (2014): यह नीति जल उपयोग की प्राथमिकता तय करती है और जल स्रोतों के संरक्षण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करती है। 7.3 कृत्रिम पुनर्भरण (Artificial Recharge) प्राकृतिक पुनर्भरण के अलावा कृत्रिम उपाय भी अपनाए जा रहे हैं: • चेक डैम, परकोलेशन टैंक, जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे संरचनाओं का निर्माण कर भूजल स्तर को स्थिर रखने का प्रयास किया जा रहा है। • टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहन देकर सिंचाई में जल की बचत की जा रही है, विशेषकर मरुस्थलीय जिलों में। 7.4 जनभागीदारी (Public Participation) जल संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानने के बजाय, जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जा रहा है: • जल चेतना अभियान, विद्यालय स्तर पर जल साक्षरता कार्यक्रम, और ग्राम जल समिति जैसे प्रयासों के माध्यम से स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। • सामुदायिक निगरानी एवं जल उपयोग का सामाजिक लेखांकन भी प्रारंभिक स्तर पर लागू किया जा रहा है। 8. चुनौतियाँ (Challenges in Water Resource Management in Rajasthan) राजस्थान में जल प्रबंधन की दिशा में कई योजनाएँ और प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं, किंतु इनकी प्रभावशीलता अनेक व्यवहारिक, संरचनात्मक और नीतिगत बाधाओं से सीमित हो जाती है। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना जल संकट की समस्या पर स्थायी नियंत्रण संभव नहीं है। 1. वित्तीय संसाधनों की कमी: जल संरक्षण एवं प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण और रखरखाव हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। राजस्थान जैसे राजस्व-संवेदनशील राज्य में अधिकांश जल परियोजनाएँ वित्तीय संकट से ग्रस्त रहती हैं, जिससे अनेक योजनाएँ अधूरी रह जाती हैं या प्रभावहीन हो जाती हैं। ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को जल प्रबंधन हेतु सीमित बजट मिलने के कारण स्थानीय स्तर पर भी क्रियान्वयन बाधित होता है। 2. जनजागरूकता का अभाव: जल संकट केवल संरचनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार से भी जुड़ा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल उपयोग की आदतें अब भी असंवेदनशील और अपव्ययी हैं। लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि जल संरक्षण केवल शासन की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। जन सहभागिता तभी सार्थक होगी जब समुदायों में जल के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव विकसित हो। 3. तकनीकी विशेषज्ञता की कमी: कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, टपक सिंचाई, जल लेखांकन आदि जैसे नवीन उपायों के प्रभावी संचालन हेतु तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। लेकिन, राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान की पहुँच सीमित है। जलग्रहण क्षेत्र विकास, भूजल विश्लेषण, GIS आधारित जल प्रबंधन जैसी तकनीकों का व्यापक उपयोग अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। 4. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: नीतिगत रूप से जल को प्राथमिकता देने की घोषणा तो की जाती है, किंतु इसका वास्तविक परिलक्षण बजट आवंटन, क्रियान्वयन निगरानी और योजना की निरंतरता में नहीं दिखाई देता। अनेक जल परियोजनाएँ केवल कागज़ी स्तर पर रहती हैं या चुनावी लाभ के लिए आंशिक रूप से लागू की जाती हैं। स्थायी जल नीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। 5. पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रबंधन में तालमेल का अभाव: राजस्थान की पारंपरिक जल संस्कृति अत्यंत समृद्ध रही है, लेकिन आधुनिक योजनाओं में इन प्रणालियों को या तो उपेक्षित किया गया है या उनके साथ समन्वय स्थापित नहीं किया गया। जोहड़, टांके, बावड़ियाँ जैसे परंपरागत साधन समाज से दूर होते गए और उनकी मरम्मत या पुनरुद्धार की योजनाएँ भी आधुनिक तकनीकों से जुड़ नहीं पाईं। यह ज्ञान-विच्छेद (knowledge gap) नीति और क्रियान्वयन के बीच दूरी बढ़ाता है। 9. सुझाव (Suggestions for Sustainable Water Management in Rajasthan) राजस्थान के जल संकट का समाधान केवल संरचनात्मक हस्तक्षेपों से नहीं, बल्कि समन्वित, सामुदायिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ही संभव है। निम्नलिखित सुझावों के माध्यम से जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सकता है: 1. जल बजट और जल लेखांकन को ग्राम स्तर पर लागू किया जाए: प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल की उपलब्धता, उपयोग, और स्रोतों का लेखा-जोखा रखने की प्रणाली विकसित की जाए। इससे स्थानीय स्तर पर जल संतुलन की जानकारी रहेगी और अनावश्यक दोहन पर रोक लगेगी। जल लेखांकन को पंचायत राज व्यवस्था में संस्थागत रूप दिया जा सकता है। 2. जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिले: राजस्थान के विविध भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान कर उनके पुनर्विकास और संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जलग्रहण क्षेत्र विकास न केवल जल संचयन में सहायक होता है, बल्कि मिट्टी अपरदन को भी रोकता है और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होता है। 3. वर्षा जल संचयन को भवन निर्माण की अनिवार्य शर्त बनाया जाए: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए भवनों, स्कूलों, अस्पतालों, पंचायत भवनों, एवं निजी घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना अनिवार्य की जानी चाहिए। इससे सतही बहाव से जल का नुकसान रुकेगा और भूजल स्तर में सुधार आएगा। 4. विद्यालय स्तर पर जल साक्षरता अभियान शुरू किया जाए: जल संरक्षण को एक सामाजिक संस्कृति के रूप में विकसित करने के लिए विद्यालयों में जल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। छात्रों के माध्यम से परिवार और समुदाय में जल के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है। इस दिशा में जल संरक्षण से जुड़ी पाठ्यवस्तु का समावेश शिक्षा नीति में किया जाना चाहिए। 5. वनों की पुनर्स्थापना द्वारा जल संतुलन में सहायता ली जाए: वनस्पति आवरण में वृद्धि जल संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख माध्यम है। जलग्रहण क्षेत्रों, पर्वतीय ढलानों और शुष्क ज़मीनों पर वृक्षारोपण कर वर्षा जल को भूमि में अवशोषित होने में मदद मिलती है, जिससे भूजल स्तर भी सुधरता है। यह प्रयास मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। 10. निष्कर्ष (Conclusion) राजस्थान में जल संसाधनों की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और संवेदनशील है। सीमित वर्षा, असमान भौगोलिक वितरण, और बढ़ती जल मांग ने राज्य को गंभीर जल संकट की ओर धकेल दिया है। इस संकट की जड़ें केवल प्राकृतिक सीमाओं में नहीं हैं, बल्कि मानवजनित गतिविधियाँ, नीति संबंधी खामियाँ, पारंपरिक प्रणालियों की उपेक्षा और तकनीकी जागरूकता की कमी भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। राज्य की जल संरचना मुख्यतः भूजल पर आधारित है, लेकिन अनियंत्रित दोहन के कारण कई जिलों में भूजल स्तर अत्यंत नीचे चला गया है। सतही जल स्रोत जैसे नदियाँ और झीलें सीमित हैं, जिनमें से अधिकांश मौसमी हैं या प्रदूषण व अतिक्रमण से प्रभावित हैं। जल संसाधनों के इस असंतुलित उपयोग ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय ढाँचे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि राजस्थान में जल प्रबंधन की वर्तमान रणनीतियाँ जैसे ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान’, ‘जल जीवन मिशन’, पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार, और कृत्रिम पुनर्भरण तकनीकें सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, किंतु उनका दायरा और प्रभावशीलता अब भी सीमित है। वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, जनजागरूकता की न्यूनता, तथा पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के बीच तालमेल की कमी इन प्रयासों को बाधित करती है। सतत जल प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है कि ग्राम स्तर पर जल बजट और जल लेखांकन को अपनाया जाए, जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण प्राथमिकता बने, और जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। स्कूलों से लेकर पंचायतों तक जल साक्षरता अभियान चलाए जाएँ और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जाए। साथ ही, वनों की पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण की रोकथाम और भूजल के वैज्ञानिक पुनर्भरण को दीर्घकालिक रणनीतियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि जल संकट कोई अपरिहार्य प्राकृतिक परिणाम नहीं, बल्कि एक सामाजिक-प्रशासनिक चुनौती है, जिसे सामूहिक भागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि राजस्थान को जल संकट से उबारना है, तो नीति निर्माण से लेकर व्यवहारिक क्रियान्वयन तक एक भौगोलिक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य होगा। 11. संदर्भ (References) 1. Government of Rajasthan. (2020). Rajasthan Water Resource Policy. Jaipur: Department of Water Resources. pp. 14–31. 2. Central Ground Water Board (2021). Dynamic Ground Water Resources of India. Ministry of Jal Shakti. pp. 56–78. 3. Singh, R.L. (2018). India: A Regional Geography. Varanasi: National Geographical Society of India. pp. 234–248. 4. UNDP India. (2019). Water Conservation Practices in Arid Regions. New Delhi. pp. 45–61. 5. Sharma, D. (2021). "Water Crisis in Rajasthan: Challenges and Opportunities." Journal of Environmental Studies, Vol. 9(2), pp. 112–126. 6. National Institute of Hydrology (NIH). (2018). Rainwater Harvesting and Groundwater Recharge in Rajasthan. Roorkee. pp. 11–25, 63–71. 7. Jain, S.K. & Kumar, R. (2020). "Traditional Water Systems in Western Rajasthan: A Study of Indigenous Techniques." Indian Journal of Geography and Environment, Vol. 25. pp. 87–101. 8. Ministry of Jal Shakti, Government of India. (2022). Annual Report on Water Resources Management. New Delhi. pp. 59–73, 121–132. 9. World Bank Report. (2019). Water Scarcity and Management Strategies in Indian Arid Zones. pp. 33–49, 90–98. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 7, July 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
Share this

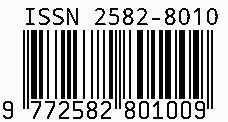
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

