
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 1
January 2026
Indexing Partners
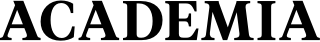




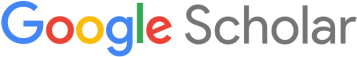








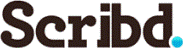




राजस्थान की नदियों और झीलों का भू-आकृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक महत्व: एक समग्र अध्ययन"
| Author(s) | Ayush Soni |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अपनी विषम जलवायु, विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र और सीमित जल संसाधनों के कारण विशेष पहचान रखता है। यहाँ का अधिकांश भूभाग शुष्क एवं अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, जहाँ जल की उपलब्धता न केवल प्राकृतिक संसाधन के रूप में, बल्कि सामाजिक अस्तित्व और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे परिदृश्य में नदियाँ और झीलें राजस्थान की जीवनरेखा के रूप में कार्य करती हैं, जिनका महत्व केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्र की भू-आकृति, पारिस्थितिकी, आजीविका, संस्कृति और पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान की नदियाँ मुख्यतः मौसमी प्रवृत्ति की हैं, जो वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। स्थायी नदियों की संख्या सीमित है, जिनमें चंबल, बनास, लूणी प्रमुख हैं। इन नदियों ने राज्य की स्थलाकृति को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कृषि, सिंचाई, और जैव विविधता के लिए आधार प्रदान किया है। वहीं दूसरी ओर, पिछोला, फतेहसागर, पुष्कर, सम्भर, जयसमंद, और राजसमंद जैसी झीलें, जो अधिकतर मानव निर्मित या प्राकृतिक अवसादों में विकसित हुई हैं, न केवल जल संचयन के प्रमुख साधन हैं, बल्कि पर्यटन, संस्कृति, और नगर नियोजन में भी योगदान देती हैं। इन जल निकायों का प्रभाव सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन के अनेक पहलुओं पर परिलक्षित होता है। उदाहरणस्वरूप, उदयपुर की झीलें नगर की स्थापत्य और पर्यटन की रीढ़ हैं, सम्भर झील भारत के प्रमुख लवण उत्पादन केंद्रों में एक है, जबकि पुष्कर झील धार्मिक आस्था और तीर्थाटन का प्रमुख केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, इन जल निकायों के आसपास की बस्तियाँ, आजीविकाएँ और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियाँ इस बात की साक्षी हैं कि राजस्थान में जल संसाधनों का सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कितना गहन महत्व है। इस शोध-पत्र में राजस्थान की नदियों और झीलों का भू-आकृतिक विश्लेषण किया गया है, जिसमें उनके उत्पत्ति स्थल, प्रवाह क्षेत्र, जलग्रहण संरचना, और स्थलाकृति पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया गया है। साथ ही, इन जल निकायों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक आयामों जैसे कृषि, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, धार्मिक गतिविधियाँ और मानव बस्तियों के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वर्तमान संदर्भ में, जब जल संकट, शहरीकरण, और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तब इन जल संसाधनों के महत्व को समग्र और बहुस्तरीय दृष्टिकोण से समझना और उनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह अध्ययन न केवल राजस्थान के जल निकायों की भौगोलिक और मानवशास्त्रीय समझ को सुदृढ़ करता है, बल्कि जल प्रबंधन एवं क्षेत्रीय विकास की रणनीतियों के लिए एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार भी प्रस्तुत करता है। 2. शोध की आवश्यकता (Need of the Study) राजस्थान में जल संसाधनों की उपलब्धता और वितरण अत्यंत विषम और असंतुलित है। राज्य का एक बड़ा भूभाग शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र में आता है, जहाँ वर्षा अल्प और अनिश्चित होती है। ऐसे परिदृश्य में सतही जल स्रोतों—विशेषकर नदियों और झीलों—का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश, इन जल निकायों की संख्या सीमित है और जो उपलब्ध हैं, वे भी वर्तमान में अतिक्रमण, जल प्रदूषण, अवैज्ञानिक शहरीकरण और जलग्रहण क्षेत्रों के क्षरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अनेक झीलें सिकुड़ती जा रही हैं, नदियाँ मौसमी होकर सूखने की कगार पर हैं, और पारंपरिक जल संरचनाएँ उपेक्षा का शिकार हैं। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि राजस्थान की नदियों और झीलों का एक भूगोल-आधारित, बहुस्तरीय और समग्र मूल्यांकन किया जाए, जिसमें न केवल उनकी उत्पत्ति, प्रवाह दिशा, और स्थलाकृति पर प्रभावों का विश्लेषण हो, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों को भी समान रूप से समझा जाए। यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जल निकायों की भौगोलिक स्थिति, आकार, और विस्तार मानव बस्तियों, कृषि प्रणाली, स्थानीय व्यवसायों और धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों को गहराई से प्रभावित करता है। इस शोध की आवश्यकता इसलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि जल स्रोतों और मानव क्रियाकलापों के बीच परस्पर क्रिया (interaction) अब केवल उपयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह पारिस्थितिकीय संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और आजीविका असुरक्षा का कारण भी बन रही है। विशेष रूप से झीलों के किनारे बसे शहरों जैसे उदयपुर, अजमेर, और जयपुर में यह परिलक्षित होता है कि यदि जल निकायों का वैज्ञानिक प्रबंधन न किया जाए, तो न केवल जल संकट गहराता है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी संकट में आ जाती है। इसके अतिरिक्त, जल निकायों के पारंपरिक उपयोग और आधुनिक उपयोग के बीच संतुलन बनाना अब एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। जब एक ओर स्थानीय समाज पारंपरिक रीति-रिवाजों, पूजा-पद्धतियों और मेला-उत्सवों में झीलों व नदियों की भूमिका को आज भी जीवंत रखे हुए है, वहीं दूसरी ओर, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और पर्यटन का दबाव इन जल निकायों की पारिस्थितिकी को क्षति पहुँचा रहा है। अतः इस द्वैत को समझना और समाधान प्रस्तुत करना इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य बनता है। इसलिए यह अध्ययन न केवल जल निकायों के भू-आकृतिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, बल्कि इनके माध्यम से स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकास, जल सुरक्षा, और संस्कृति संरक्षण को जोड़ने वाली रणनीतियाँ तैयार करने हेतु भी अनिवार्य है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह शोध और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यह भविष्य में जल प्रबंधन और जल संरक्षण की दिशा में नीति निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और स्थानीय समुदायों को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। 3. उद्देश्य (Objectives) इस शोध का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में स्थित नदियों और झीलों के भू-आकृतिक स्वरूप तथा उनके सामाजिक-आर्थिक योगदान का समग्र विश्लेषण करना है। विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदु इस अध्ययन के केंद्र में हैं: 1. राजस्थान की प्रमुख नदियों और झीलों की भौगोलिक स्थिति, प्रवाह मार्ग, और भू-आकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना। 2. इन जल निकायों के आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना। 3. जल निकायों के पारंपरिक उपयोग (जैसे धार्मिक, सिंचाई, लोक-आस्थाएँ) और आधुनिक उपयोग (जैसे शहरी जल आपूर्ति, पर्यटन, उद्योग) के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना। 4. नदियों और झीलों से जुड़े पर्यावरणीय संकटों जैसे अतिक्रमण, प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान करना। 5. जल निकायों के सतत संरक्षण और प्रबंधन के लिए व्यवहारिक, समन्वित और सहभागी सुझाव प्रस्तुत करना। 4. अध्ययन क्षेत्र का परिचय (Overview of Study Area) राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य विविधतापूर्ण और जटिल है। राज्य का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला से घिरा है, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग थार मरुस्थल से आच्छादित है, जो अत्यंत शुष्क और रेत के विस्तार वाला क्षेत्र है। दक्षिण-पूर्व में चंबल नदी क्षेत्र स्थित है, जो एकमात्र स्थायी जल निकासी वाला क्षेत्र है। राज्य की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जो वर्षा ऋतु में सक्रिय होती हैं और शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। झीलें या तो भूगर्भीय अवसादों में बनी हैं या ऐतिहासिक रूप से मानव निर्मित जल संरचनाओं के रूप में विकसित की गई हैं। इनमें से कई झीलें और नदियाँ आज शहरीकरण, प्रदूषण और जलग्रहण क्षेत्र क्षरण से संकटग्रस्त हैं। प्रमुख नदियाँ: • चंबल नदी – राज्य की एकमात्र बारहमासी नदी, जो कोटा, बाराँ और सवाई माधोपुर जिलों से प्रवाहित होती है। • बनास नदी – अरावली से निकलकर पूर्वी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बहती है और चंबल की सहायक है। • लूणी नदी – पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी मौसमी नदी, जिसका जल खारा होता है और जो अंतर्देशीय रूप से रन ऑफ कच्छ में लुप्त हो जाती है। प्रमुख झीलें: • पिछोला एवं फतेहसागर झील (उदयपुर) – स्थापत्य सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। • पुष्कर झील (अजमेर) – धार्मिक महत्व की प्राचीन झील। • सम्भर झील (जयपुर-नागौर सीमा) – भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी जल की झील, लवण उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। यह विविध परिदृश्य इस अध्ययन को एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। 5. भू-आकृतिक महत्व (Geomorphological Significance) राजस्थान की नदियाँ और झीलें राज्य की स्थलाकृति और पर्यावरणीय संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन जल निकायों ने जहाँ एक ओर धरातलीय आकृतियों जैसे घाटियाँ, अवसाद क्षेत्र, नदी तल और निक्षेपण मैदान बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मृदा गठन, वनस्पति वितरण, और स्थानीय जलवायु नियंत्रण में भी योगदान दिया है। प्रमुख भू-आकृतिक विशेषताएँ: • चंबल नदी की गॉर्ज (Gorge) और रैवीन (Ravine) संरचना विशेष भूगर्भीय घटनाओं का परिणाम हैं। यह क्षेत्र चंबल घाटी में अत्यंत गहराई तक कटाव द्वारा निर्मित हुआ है और भू-आकृतिक अध्ययन का विशिष्ट उदाहरण है। • लूणी नदी प्रणाली थार मरुस्थल की अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली (inland drainage) का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे जवाई, सुकड़ी और बंडई भी अस्थायी जलधाराएँ हैं, जो रेतीले मैदानों और खारी मैदानों से होकर बहती हैं। • सम्भर झील, जो एक टेक्टोनिक अवसाद में स्थित है, भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है। यह झील नमक उत्पादन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसका भू-आकृतिक अध्ययन भी कई महत्वपूर्ण भूगर्भीय परिकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। • झीलों के किनारे बने निक्षेपण क्षेत्र (Deposition Zones) और दलोआन भूमि (Marshy Plains) जल संचयन और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। इन सभी विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान की जल प्रणालियाँ केवल जल के स्रोत नहीं हैं, बल्कि राज्य की भू-आकृतिक विविधता, स्थानीय पर्यावरण, और प्राकृतिक संतुलन को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। 6. सामाजिक-आर्थिक महत्व (Socio-Economic Significance) राजस्थान की नदियाँ और झीलें केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना, आजीविका, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन का आधार भी हैं। इन जल निकायों के चारों ओर मानव जीवन की अनेक गतिविधियाँ संचालित होती हैं जो क्षेत्रीय विकास को गहराई से प्रभावित करती हैं। 1. कृषि और सिंचाई राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र शुष्क होने के कारण सिंचाई के लिए सतही जल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर है। चंबल नदी पर आधारित सिंचाई परियोजनाएँ—जैसे चंबल परियोजना—ने कोटा, बाराँ और बूंदी जैसे जिलों की कृषि उत्पादकता को नई ऊँचाइयाँ दी हैं। इसी प्रकार बनास और लूणी नदियाँ अपने-अपने क्षेत्र में सिंचाई और स्थानीय जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। झीलों के जल का उपयोग भी शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में बागवानी व कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। 2. मत्स्य पालन और लवण उत्पादन राजस्थान की झीलें, विशेषकर सम्भर झील, भारत के सबसे बड़े लवण (साल्ट) उत्पादन केंद्रों में एक है, जहाँ हजारों परिवारों की आजीविका इस पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त पिछोला, फतेहसागर, जयसमंद जैसी झीलें मत्स्य पालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और पोषण सुरक्षा दोनों प्राप्त होती है। 3. पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व राजस्थान की झीलें न केवल पर्यावरणीय बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। पुष्कर झील हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में एक है, जहाँ कार्तिक मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। उदयपुर की झीलें—पिछोला, फतेहसागर, और स्वरूप सागर—राज्य को "झीलों का शहर" की उपाधि दिलाती हैं और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र हैं। इन झीलों के किनारे स्थित महल, मंदिर और घाट न केवल स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी करते हैं। 4. जलापूर्ति और जीवन निर्वाह राज्य के अनेक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र इन जल स्रोतों पर अपनी पेयजल आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर, जयपुर शहर की जल आपूर्ति आंशिक रूप से सम्भर और रामगढ़ जलाशयों से होती है, वहीं अजमेर और उदयपुर जैसे नगरों में भी झीलें जल आपूर्ति का स्रोत हैं। ये जल निकाय जीवन निर्वाह की बुनियादी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। 7. चुनौतियाँ (Challenges) हालाँकि राजस्थान की नदियाँ और झीलें सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी ये अनेक संकटों से जूझ रही हैं। इन जल निकायों के संरक्षण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएँ हैं: 1. जल निकायों का अतिक्रमण और अनियंत्रित शहरीकरण – झीलों और नदी किनारों पर अतिक्रमण के कारण उनके आकार में कमी आई है और पारिस्थितिक संतुलन बाधित हुआ है। 2. प्रदूषण का बढ़ता स्तर – घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, और धार्मिक कचरे से झीलें और नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। 3. मौसमी निर्भरता और जल की मात्रा में कमी – अधिकांश नदियाँ मौसमी होने के कारण गर्मियों में सूख जाती हैं, जिससे जल संकट उत्पन्न होता है। 4. भूगर्भीय जल पुनर्भरण में कमी – सतही जल स्रोतों की गिरावट के कारण भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। 5. नीतिगत उपेक्षा और समन्वयहीन प्रबंधन – जल निकायों के संरक्षण हेतु स्पष्ट और प्रभावी नीति का अभाव, तथा विभागीय समन्वय की कमी। 8. सुझाव (Suggestions) राजस्थान की नदियों और झीलों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए बहुआयामी और समन्वित रणनीतियों की आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझाव व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं: 1. भूगोल-आधारित जल प्रबंधन नीति तैयार की जाए, जो प्रत्येक नदी और झील की भौगोलिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर संरक्षण योजना बनाए। 2. झीलों के पुनर्जीवन कार्यक्रम को शहरी विकास योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि अतिक्रमण और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। 3. पर्यटन राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आरक्षित किया जाए। 4. झीलों और नदियों के चारों ओर ग्रीन बफर जोन विकसित किए जाएँ, जहाँ निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध हो। 5. जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाए – विशेष रूप से पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों जैसे जोहड़, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण हेतु समुदाय को सक्रिय भागीदारी दी जाए। 9. निष्कर्ष (Conclusion) राजस्थान की नदियाँ और झीलें, चाहे वे मौसमी हों या स्थायी, राज्य की भौगोलिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत, और आर्थिक जीवन की रीढ़ हैं। इन जल निकायों का भू-आकृतिक योगदान केवल स्थलाकृति के निर्माण में सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, मानव बसावट, कृषि पद्धतियों और सांस्कृतिक धरोहर को भी आकार दिया है। चंबल की घाटियाँ, सम्भर की लवणीय भूमि, और उदयपुर की झीलें—ये सभी उदाहरण हैं कि जल निकायों ने किस प्रकार राजस्थान की पहचान को बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है। सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी इनका प्रभाव व्यापक है—चाहे वह सिंचाई, मत्स्य पालन, लवण उत्पादन, धार्मिक पर्यटन, या शहरी जल आपूर्ति हो। ये जल निकाय अनेक समुदायों की आजीविका का माध्यम हैं और स्थानीय संस्कृति, परंपराओं एवं उत्सवों के केंद्र बिंदु भी हैं। हालांकि, आज ये अमूल्य संसाधन प्रदूषण, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और नीतिगत उपेक्षा के कारण संकट की स्थिति में पहुँच गए हैं। शहरीकरण के दबाव और पारंपरिक जल संरचनाओं की उपेक्षा ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इन जल निकायों के संरक्षण के लिए एकीकृत, समावेशी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस शोध-पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि यदि राजस्थान की नदियों और झीलों का संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित न रहकर, समाज, स्थानीय समुदायों, पर्यावरणविदों और नीति-निर्माताओं की संयुक्त भागीदारी से किया जाए, तो न केवल जल संकट से निपटा जा सकता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजस्थान की नदियाँ और झीलें केवल भौगोलिक घटक नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और विकास की धाराएं हैं, जिनका संरक्षण राज्य के सतत और समावेशी भविष्य की कुंजी है। 10. संदर्भ सूची (References) 1. शर्मा, के. एल. (2014). राजस्थान का भूगोल. जयपुर: राजस्थानी ग्रंथ अकादमी। पृष्ठ: 42–78, 103–114। 2. Government of Rajasthan. (2021). State Water Policy 2021. Department of Water Resources, Government of Rajasthan. Pages: 4–18, 33–46. 3. Singh, R.L. (2016). India: A Regional Geography. Varanasi: National Geographical Society of India. Pages: 312–340. 4. UNDP & Ministry of Jal Shakti. (2020). Water Resource Mapping of Arid and Semi-Arid Zones of India. Government of India. Pages: 58–76. 5. मेहता, एम. (2019). राजस्थान की पारंपरिक जल संरचनाएँ: एक सांस्कृतिक अध्ययन. जोधपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। पृष्ठ: 88–102। 6. Central Ground Water Board (CGWB). (2022). Annual Ground Water Report: Rajasthan State. Ministry of Jal Shakti, Government of India. Pages: 12–37. 7. Sharma, A. & Pareek, R. (2018). “Geo-environmental Analysis of Sambhar Salt Lake Region.” International Journal of Geographical Studies, Vol. 5(2), pp. 112–129. 8. Rajasthan Tourism Department. (2023). Tourism Profile: Lakes and River-based Destinations of Rajasthan. Government of Rajasthan. Pages: 7–24. 9. Bandyopadhyay, J. (2017). “Water, Ecosystem and Livelihood Linkages in Rajasthan.” Economic and Political Weekly, Vol. 52(41), pp. 58–66. 10. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC). (2020). Wetlands of India: Atlas and Policy Framework. Government of India. Pages: 133–150 (Rajasthan Chapter). 11. Chouhan, T.S. (2007). Geography of Rajasthan. Jaipur: Ravindra Publications. Pages: 94–125. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 7, July 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
Share this

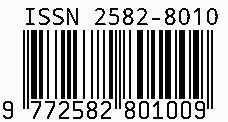
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

